भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आर्सेनिक-दूषित पानी पीते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर, ख़ास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रभावित क्षेत्रों में निजी, सुरक्षित पेयजल की माँग कम बनी हुई है। यह लेख असम में किए गए एक प्रयोग के आधार पर दर्शाता है कि किस प्रकार जल गुणवत्ता जागरूकता हस्तक्षेपों को, सरकारी लाभ प्राप्त करने में लेन-देन सम्बन्धी जटिलता को कम करने के साथ संयोजित करने से, इस समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है।
भारत और बांग्लादेश को मिलाकर, भूजल के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के सम्पर्क में आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। भारत के, ख़ास तौर पर असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के 35 जिलों में, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आर्सेनिक-दूषित पानी के सम्पर्क में हैं (शाजी एवं अन्य 2021)। आर्सेनिक से प्रभावित आबादी में से लगभग 50% बच्चे हैं और भारत में प्रति 100 जीवित जन्मों पर 30 मौतों की उच्च शिशु मृत्यु दर में एक सम्भावित कारक हैं (असदुल्लाह और चौधरी 2011)। बच्चों में वयस्कों की तुलना में कम प्रतिरक्षा क्षमता होने और उनके शरीर में पानी के अधिक अनुपात के कारण, वे आर्सेनिक विषाक्तता के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। गर्भावस्था के दौरान आर्सेनिक-दूषित पानी पीने से मृत जन्म और कई प्रतिकूल बाल विकास परिणाम भी जुड़े हैं (वतानबे एवं अन्य 2007, काइल एवं अन्य 2016)। हालांकि, माताओं के स्तनपान की अवधि और मात्रा बढ़ाकर बच्चों को आर्सेनिक से बचाना सम्भव है, क्योंकि पानी से आर्सेनिक के सम्पर्क के बावजूद माँ के दूध में आर्सेनिक की मात्रा नगण्य होती है (केस्किन, शास्त्री और विलिस 2017, गार्सिया साल्सेडो एवं अन्य 2022)।
वर्ष 2019 में, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सस्ती कीमतों पर सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति प्रदान करना था। माँग-संचालित जल आपूर्ति योजना होने के नाते, यह निजी नल के लिए आवेदन करने और बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने के लिए गाँव की जल उपयोगकर्ता समितियों और परिवारों की पहल पर निर्भर करती है। इस मॉडल के अधिकांश भारतीय राज्यों में कारगर होने की सम्भावना है, जबकि असम के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के वैकल्पिक स्रोतों की प्रचुरता (असम एक जल-अधिशेष राज्य है) और भूजल पर सांस्कृतिक निर्भरता के कारण निजी जल की माँग कम है।
ग्रामीण असम में सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले नल के पानी की माँग में कमी क्यों है? सैद्धांतिक रूप से, नल के पानी की कम माँग के कम से कम तीन कारणों के बारे में सोचा जा सकता है। पहला- परिवार स्वास्थ्य उत्पादन कार्य1 (ग्रोनौ 1997) के अपने ज्ञान के आधार पर विकल्प चुनते हैं और अगर जानकारी अधूरी है, तो परिवार उप-इष्टतम विकल्प चुन सकते हैं। इसके अनुरूप, मैडाजेविक्ज़ एवं अन्य (2007) ने पाया कि बांग्लादेश में यादृच्छिक रूप से चुने गए जिन परिवारों को बताया गया कि उनका पानी आर्सेनिक-दूषित है, तो उनके द्वारा स्रोत बदलने की सम्भावना 37% अधिक हो गई। दूसरा, गरीब परिवार आर्थिक रूप से मजबूर हो सकते हैं, जिससे जल आपूर्ति सहित घरेलू बुनियादी ढाँचे में निवेश कम हो सकता है। तीसरा, विद्युतीकरण, गैस और जल आपूर्ति जैसी ज़रूरतों तक सार्वभौमिक पहुँच वाली सरकारी योजनाओं में लेन-देन सम्बन्धी अच्छी-खासी जटिलताएँ होती हैं, जो परिवारों के लिए बहुत बोझिल हो सकती हैं (ब्लैंकेनशिप एवं अन्य 2020)। जहाँ पानी के वैकल्पिक सस्ते स्रोत उपलब्ध नहीं हैं और लोगों को पानी तक पहुँचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, उन क्षेत्रों में तरलता की बाधाएँ पानी की गुणवत्ता की माँग के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, जबकि यह उस क्षेत्र के सन्दर्भ में बाधा नहीं है जिस पर हम अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 76वें दौर के अनुसार, भारत में 10.5%ग्रामीण परिवार पानीइकट्ठा करने में औसतन 30 मिनट से अधिक समय व्यतीत करते हैं जबकि असम में यह औसत 10 मिनट है और जो देश में सबसे कम है। इसलिए, अपने अध्ययन में हम दो शेष बाधाओं, अर्थात् सूचना और लेन-देन लागतों पर ध्यान केन्द्रितकरते हैं।
प्रयोग
नवंबर 2021 में हमने असम के जोरहाट जिले के तिताबोर ब्लॉक में एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) के साथ भागीदारी की। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, तिताबोर के पानी में आर्सेनिक की मात्रा 194 से 491 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के बीच है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित मात्रा सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से बहुत अधिक है और यहाँ की अधिकांश आबादी पानी की ज़रूरतों के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल पर निर्भर है। एनएचएम ने, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा)2 द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर, तिताबोर में छोटे बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं वाले परिवारों की सूची प्रदान की। हस्तक्षेप के तहत 80 से अधिक गाँवों में रहने वाले कुल 2,064 परिवारों को यादृच्छिक रूप से एक 'नियंत्रण' समूह (कोई हस्तक्षेप नहीं) और दो उपचार समूहों, ‘सूचना उपचार’ तथा 'सूचना प्लस लेन-देन लागत' में विभाजित किया गया था।
‘सूचना समूह’ को स्थानीय भाषा में एक वीडियो दिखाया गया जिसमें उन्हें भूजल में व्याप्त आर्सेनिक, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर आर्सेनिक के स्वास्थ्य प्रभाव, सुरक्षित पेयजल के वैकल्पिक स्रोतों और आर्सेनिक-दूषित पानी के सम्पर्क से छोटे बच्चों को बचाने के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे ‘उपचार समूह’ को वीडियो के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी और निजी सरकारी आपूर्ति वाले पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें आवेदन पत्र भरने और दाखिल करने में भी मदद की गई।
मुख्य परिणाम
उपचार से आर्सेनिक के बारे में जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि हुई और केवल सूचना उपचार ही जल सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने में वृद्धि के लिए पर्याप्त था- सामुदायिक नल के पानी, वर्षा जल संचयन या बोतलबंद पानी के उपयोग में 12 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। दिलचस्प बात यह है कि केवल संयुक्त उपचार वाले दूसरे उपचार समूह ने ‘नियंत्रण समूह’ के सापेक्ष पाइप के पानी की माँग में सकारात्मक उल्लेखनीय वृद्धि (128%) दर्शाई। इससे पता चलता है कि पानी की माँग को बढाने में केवल ‘जानकारी’ का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय, पानी की अधिक घरेलू माँग को प्रेरित करने के लिए इसे सरल कागज़ी कार्रवाई और कम जटिल प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, संयुक्त उपचार वाले दूसरे उपचार समूह में हस्तक्षेप के बाद माताओं और गर्भवती महिलाओं में स्तनपान की सम्भावना और आवृत्ति, दोनों में वृद्धि होने की अधिक सम्भावना थी। ‘संयुक्त’ हस्तक्षेप के लिए, स्तनपान की सम्भावना 4 प्रतिशत अंकों से बढ़ी और नियोजित स्तनपान की अवधि 2.6 महीने बढ़ गई। हालांकि दोनों ‘उपचार’ समूहों की महिलाएं स्तनपान के लाभों का मूल्याँकन करने में सक्षम थीं, ‘संयुक्त उपचार’ समूह में स्तनपान संबंधित व्यवहार प्रभावित हुआ क्योंकि सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने की समय लागत के बारे में अधिक जागरूक होने से महिलाएं अब समय की लागत का मूल्याँकन करने में सक्षम थीं।
अंत में, हमने पाया कि सूचना हस्तक्षेप के बाद महिला-प्रधान परिवारों और कम आय वाले परिवारों को उनके बच्चों के बीमार होने के बारे में पता चलने की सम्भावना बढ़ी थी। हमारे हस्तक्षेप से गरीब परिवारों में पानी के लिए भुगतान करने की इच्छा में भी वृद्धि हुई।
नीतिगत निहितार्थ
हमारे परिणाम सरकारी जल आपूर्ति योजनाओं को अपनाने में वृद्धि लाने के लिए एक सरल लागत प्रभावी रणनीति की ओर इशारा करते हैं। कागज़ी कार्रवाई एवं आवेदन जमा करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के माध्यम से, लेन देन लागत में कमी को जल गुणवत्ता सम्बन्धी जागरूकता के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है। इससे सार्वजनिक जल योजनाओं की माँग बढ़ाने और इच्छित लाभार्थियों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने में मदद मिलेगी।
टिप्पणी:
- स्वास्थ्य उत्पादन कार्य एक ऐसा कार्य है जो विभिन्न कारकों (जैसे शिक्षा, आय, सूचना स्तर, इत्यादि) का किसी व्यक्ति या परिवार के स्वास्थ्य पर अधिकतम प्रभाव दर्शाता है।
- आशाएँ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आमतौर पर महिलाएँ, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में नियुक्त किया जाता है।
अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।
लेखक परिचय: रश्मि बरुआ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास केंद्र में काम करती हैं। उनके शोध क्षेत्रों में शिक्षा और श्रम अर्थशास्त्र शामिल हैं, जिसमें से लिंग, प्रारंभिक बचपन, मानव पूंजी निवेश (स्वास्थ्य और शिक्षा) और महिला श्रम आपूर्ति में उनकी विशेष रुचि है। देबोष्मिता ब्रह्मा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में शोधार्थी हैं। वह एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री हैं, जिसकी रुचि लिंग, पर्यावरण और विकास अध्ययन में है। प्रार्थना अग्रवाल गोयल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। वह भी एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री हैं जिसकी रुचि लिंग, अपराध, पर्यावरण और विकास अध्ययन के क्षेत्रों में है।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।




 19 जून, 2024
19 जून, 2024 


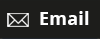



Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.