हमारे संस्थापक प्रधान संपादक अशोक कोतवाल की याद में वर्ष 2022 में ‘अशोक कोतवाल स्मृति व्याख्यान’ की शुरुआत विकास के प्रमुख मुद्दों पर एक वार्षिक व्याख्यान के रूप में की गई थी। 11 दिसंबर 2024 को संपन्न इस व्याख्यान के तीसरे संस्करण में, प्रोफेसर रोहिणी पांडे ने स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संबंधित चुनौतियों और अवसरों के बारे में बात की। इस व्याख्यान की रिकॉर्डिंग अब विडियो प्रारूप में उपलब्ध है।
प्रोफेसर रोहिणी पांडे ने अपने व्याख्यान की शुरुआत वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए की, जिसका उद्देश्य देशों को 2050 तक शुद्ध शून्य-कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ना था ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°सेल्सियस से कम पर सीमित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया जा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की ज़िम्मेदारी किसकी बनती है। कम आय वाले देश अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने में जुटे होने के कारण उनके द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की सम्भावना कम है। साथ ही वैश्विक जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस के हित में अमीर देशों को कार्बन के मामले में 'नेगेटिव' होना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि वर्तमान में वैश्विक लक्ष्य पूरे होने से बहुत दूर हैं और हम 2°सेल्सियस की सीमा से बहुत ऊपर हैं। जब घरेलू नीतियों की बात आती है, तो कार्बन से जुड़े कर वैश्विक उत्सर्जन के केवल 6% को कवर करते हैं। हालांकि कार्बन अनुपालन बाज़ार उत्सर्जन के 19% को कवर करते हैं, लेकिन इन नीतियों को कितना बढ़ाया जा सकता है, इसकी एक सीमा है।
इसलिए प्रो. पांडे ने समग्र उत्सर्जन को कम करने के लिए, रोके गए उत्सर्जन (उत्सर्जन जो नहीं हुआ) पर एक तंत्र के रूप में ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। चूंकि उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई का उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उन्होंने इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार मौजूदा वनों, विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों में स्थित वनों को, वन-आवरण बनाए रखने के लिए भुगतान के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। चूंकि निम्न आय वाले देश उत्सर्जन को कम करने के सबसे आसान स्थान हैं, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक जलवायु वित्त को इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। लागत में इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि निम्न आय वाले देशों को औद्योगीकरण का एक अलग रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी। क्योंकि कोई भी देश पर्याप्त ऊर्जा उपयोग के बिना आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकता और जैसे-जैसे देश अमीर होते जाते हैं, वे अधिक तेज़ी से वनों की कटाई करते हैं।
व्याख्यान में आगे निम्न आय वाले देशों में उत्सर्जन को कम करने के संभावित तंत्रों पर चर्चा हुई। पहला ‘कार्बन सीमा समायोजन तंत्र’ है, जिसे कम या बिना घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण वाले देशों से आयात में निहित उत्सर्जन पर कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, प्रोफेसर पांडे ने कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है क्योंकि इसका बोझ निर्यातक देश पर पड़ता है। एक अन्य दृष्टिकोण में ‘कार्बन ऑफसेट ट्रेडिंग’ के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करना शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए तीन प्रमुख तरीके- उत्सर्जन से बचना, उत्सर्जन को कम करना, तथा CO2 को हटाना और संग्रहित करना- न केवल समतापूर्ण हैं, बल्कि उनके समर्थन में दक्षता संबंधी तर्क भी मौजूद हैं।
प्रोफेसर पांडे ने चर्चा को प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ बुनियादी शब्दावली प्रस्तुत की- उन्होंने कार्बन ऑफसेट क्रेडिट, जिसका कारोबार स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों (वोलंटरी कार्बन मार्केट- वीसीएम) में होता है, और कार्बन परमिट क्रेडिट, जिसका कारोबार विनियमित अनुपालन बाज़ारों (कंप्लायंस मार्केट) में होता है, के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बाज़ारों को समझना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जिसने देश के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और फर्मों के कार्यों के बीच तनाव को देखते हुए सीओपी29 के तहत अनुपालन बाज़ार तंत्र को अपनाया है। वनों के बारे में बहुत-सी सोच एनडीसी को पूरा करने के संदर्भ में है, न कि इस बारे में कि भूमि-उपयोग वाली परियोजनाएं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में कैसे प्रवेश करेंगी।
आगे, व्याख्यान में स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों, वीसीएम, की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। आज, वीसीएम वैश्विक उत्सर्जन का केवल 0.2% कवर करते हैं, फिर भी, ये बाज़ार न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्तपोषण के लिए एक अवसर प्रस्तुत करते हैं। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि अर्थशास्त्री इससे जुड़े मुद्दों के बारे में विचार कर सकते हैं। उन्होंने वीसीएम में चार प्रमुख कारकों को रेखांकित किया- खरीदार, जो आमतौर पर ऊर्जा-गहन कंपनियां होती हैं ; आपूर्तिकर्ता, जैसे कि परियोजना डेवलपर्स ; दलाल, जो परियोजना डेवलपर्स से कार्बन अनुमतियों की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं और केंद्र, जो कार्बन ऑफसेट पर निगरानी रखते हैं और सत्यापित करते हैं। वीसीएम में भारत की भागीदारी ज्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के रूप में है, भूमि उपयोग परियोजनाओं के रूप में नहीं। देश में विचारार्थ पंजीकृत परियोजनाओं का एक बड़ा हिस्सा है। यहां 500 से अधिक परियोजना डेवलपर्स हैं, तथा भारत ने अधिकतम संख्या में क्रेडिट ‘रिटायर’ किए हैं यानी उन्हें बाज़ार से हटाकर हमेशा के लिए सुरक्षित रखा है।
वर्ष 2021 तक, वीसीएम में जीवाश्म ईंधन और ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से पर्याप्त मांग के साथ उल्लेखनीय उछाल आया। हालांकि, 2021 के बाद, दो कारणों से बाज़ार में गिरावट आई। पहला, बाज़ार में बेची जा रही परियोजनाओं की गुणवत्ता के बारे में चिंता के कारण मांग में स्थिरता, और दूसरा, शोध परिणामों का जारी होना, जिसमें बताया गया कि कई परियोजनाएं ‘अतिरिक्त या एडिशनल’ नहीं थीं। प्रो.पांडे ने आगे बताया कि ‘अतिरिक्तता या एडिशनेलिटी’ इस बाज़ार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थ है कि यदि आपने इस परियोजना के लिए पैसे नहीं दिए होते, तो उत्सर्जन में यह कमी नहीं हुई होती। यदि ‘नॉन-एडिशनल’ परियोजनाओं का उपयोग कंपनियों द्वारा अपने उत्सर्जन को और बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका अर्थ होगा कि बाज़ार ने वैश्विक उत्सर्जन में कमी करने के बजाय इसमें समग्र वृद्धि को उचित ठहराया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वो परियोजना डेवलपर्स जो वैसे भी जंगल नहीं काटते, उनके लिए बाज़ार में प्रवेश करना सबसे सस्ता है- वे अपने कार्यों में कोई बदलाव किए बिना ही पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा, सत्यापनकर्ताओं को गैर-अतिरिक्तता या नॉन-एडिशनेलिटी वाली परियोजनाओं की स्क्रीनिंग करनी होती है और उन्हें परियोजना को पास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें परियोजना के सत्यापित होने के आधार पर भुगतान किया जाता है।
तो वीसीएम का क्या भविष्य है? प्रो. पांडे ने तर्क दिया कि ‘गैर-अतिरिक्तता’ को हल करना एक कठिन समस्या होने के बावजूद, ‘अच्छे खरीदारों’ की इसमें बहुत रुचि है। ये विशेष रूप से गूगल, मेटा इत्यादि जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कम्पनियां हैं, जो अपने डेटा केंद्रों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं और हितधारकों की ओर से काफी दबाव का सामना कर रही हैं। स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार के लिए इंटीग्रिटी काउंसिल (आईसीवीसीएम) पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। हालांकि, ऐसा निकाय केवल सिद्धांत निर्धारित कर सकता है। ऐसे मानकों और प्रतितथ्यों पर शोध की आवश्यकता है जो सार्थक हों।
प्रो. पांडे ने तीन संस्थागत चुनौतियों को रेखांकित किया, जिनका समाधान किया जाना चाहिए। पहला है समानता का मुद्दा। दुनिया में शेष उत्सर्जन क्षेत्र की कुल कमी को देखते हुए, जलवायु न्याय की आवश्यकता है कि निम्न आय वाले देशों को इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा मिले। वर्तमान वीसीएम ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें केवल दो पक्षों के बीच ‘ऑफ-द-काउंटर’ व्यापार शामिल है। दूसरा, बेहतर गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट की आवश्यकता है, जो इस बारे में सवाल उठाता है कि परियोजनाओं द्वारा अतिरिक्त कार्बन कटौती के मापन के कौन से नियम होने चाहिए। तीसरा पहलू कार्बन बिक्री का सत्यापन और इसके लिए प्रभावी निगरानी तंत्र का होना है।
प्रो. पांडे के अनुसार, निष्पक्ष तरीके से नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें अंततः वैश्विक उत्तर की कंपनियों और वैश्विक दक्षिण के परियोजना डेवलपर्स की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ एक नए अनुपालन बाज़ार की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। वैश्विक उत्तर की कंपनियां स्वयं के उत्सर्जन में कमी लाने तथा डेवलपर्स के माध्यम से उत्सर्जन में कमी लाने के संयोजन का उपयोग करते हुए समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेदार होंगी। अर्थशास्त्रियों और अन्य लोगों को जिन सवालों के बारे में सोचना चाहिए, वे हैं कंपनियों और डेवलपर्स का सही अनुपात क्या हो, तथा जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए परमिट किस प्रकार आवंटित किए जाएं। अंत में, प्रो. पांडे ने इस तरह के बाज़ार में भूमि उपयोग संबंधी परियोजनाओं को शामिल करने के महत्व को दोहराया, जिसमें उपग्रह चित्रण और रिमोट सेंसिंग जैसी प्रौद्योगिकियां ‘अतिरिक्तता’ के मुद्दे को हल करने में मदद करेंगी।
व्याख्यान के बाद श्रोताओं के साथ दिलचस्प चर्चा हुई, जिसमें प्रोफेसर पांडे से वनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कार्बन क्रेडिट और भुगतान को बढ़ाने में आने वाली मूलभूत चुनौतियों से लेकर प्रकृति-आधारित समाधानों में कार्बन के समय-मूल्य को शामिल करने तथा वनों की कटाई, ऊर्जा खपत व कृषि से होने वाले उत्सर्जन के बीच अंतर करने जैसे मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए। अंग्रेज़ी में प्रश्न व उत्तर नीचे उपलब्ध हैं :
अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें। मूल विडिओ के हिन्दी सबटाइटल्स उपलब्ध हैं। उन्हें देखने के लिए आप यूट्यूब की सेटिंग में सबटाइटल्स के विकल्प को ऑन करने के बाद, हिन्दी भाषा चुनिए।
लेखक परिचय : रोहिणी पांडे येल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की हेनरी जे हाइन्ज़ द्वितीय प्रोफेसर और आर्थिक विकास केंद्र की निदेशक हैं। इससे पहले वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में सार्वजनिक नीति की मोहम्मद कमाल प्रोफेसर, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष, नीति डिजाइन के लिए साक्ष्य के सह-निदेशक और सतत विकास समूह के लिए शासन नवाचारों की निदेशक थीं। वे आर्थिक विकास पर शोध ब्यूरो (बीआरईएडी) की कार्यकारी समिति की सदस्य हैं, जमील गरीबी कार्रवाई प्रयोगशाला (जेपीएएल) में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सरकार समूह की सह-अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (एनबीईआर) में एक शोध सहयोगी हैं। उनका शोध इस बात की जांच करता है कि लोकतांत्रिक संस्थानों और सरकारी विनियमन का डिज़ाइन नीति परिणामों और नागरिक कल्याण को कैसे प्रभावित करता है, खासकर दक्षिण एशिया में। विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रयोगों के माध्यम से उनका काम आर्थिक मॉडलों का परीक्षण करने के लिए वास्तविक दुनिया के साक्ष्य के उपयोग पर जोर देता है। उन्होंने चुनावी जवाबदेही और पारदर्शिता पहल, वित्तीय पहुँच पहल और कम आय वाले सेटिंग्स में पर्यावरण विनियमन के डिजाइन और प्रभाव पर बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्तमान परियोजनाओं में निम्नलिखित की जांच शामिल है: राजनीतिज्ञ रिपोर्ट-कार्ड के माध्यम से सूचना प्रकटीकरण; माइक्रोफाइनेंस के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव; भारत में पर्यावरण विनियमन की प्रभावकारिता; और भारत में उत्सर्जन व्यापार बाजार की लागत और लाभ। रोहिणी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में एमए और दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की है।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।




 10 फ़रवरी, 2025
10 फ़रवरी, 2025 


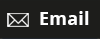


Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.