स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 से 16 जून, 1972 को आयोजित पहली पर्यावरण संगोष्ठी के परिणामस्वरूप 1973 की 5 जून को 'मात्र एक पृथ्वी' के थीम से मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस ने एक लम्बी अवधि का सफर तय कर लिया है। परन्तु क्या पृथ्वी के समस्त देशों और भारत ने भी पर्यावरण को मानव कल्याण योग्य बनाए रखने की दिशा में उतना ही लम्बा सफर तय किया है? इस महत्वपूर्ण अवसर पर I4I के प्रधान संपादक परीक्षित घोष भारत की पर्यावरण नीति, सामाजिक सुरक्षा जाल और व्यापक आर्थिक प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित करने वाले एक समग्र दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। जलवायु सम्बन्धी ज़रूरतें कब और कहाँ से उत्पन्न होंगी, इसके पूर्वानुमान में आ रही कठिनाई को देखते हुए, वे देश के लिए एक समेकित हरित निधि का विचार प्रस्तुत करते हैं।
20वीं सदी के मध्य में उपनिवेशवाद के उन्मूलन की लहर के बाद, विकास दुनिया के लिए एक नवीन मंत्र बन गया। नए राष्ट्रों ने स्वतंत्रता से ज़्यादा की मांग की। वे सम्मान की भी तलाश में थे, जो केवल पूर्वकालीन शासकों के साथ आर्थिक समानता के ज़रिए ही आ सकता था।
यह तलाश चलकर आज एक विस्तृत दायरे में पहुँच चुकी है, जो केन्द्रीय नियोजन और परिबद्ध अर्थव्यवस्थाओं की सीमाओं से निकलकर, उदार बाज़ारों और मुक्त व्यापार की ओर बढ़ रही है। फिर भी, समय के साथ-साथ नीति-निर्माताओं और जनता को यह अहसास हुआ है कि आर्थिक विकास के गम्भीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे अक्सर अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और पर्यावरण का क्षरण भी हो रहा है। इस प्रवृत्ति का एक स्पष्ट चित्र दोहरी कुज़नेट रेखाओं, ट्विन कुज़नेट कर्व (नुरोग्लू और कुंस्त 2017) में दिखाई देता है। आज यह लगभग पारम्परिक ज्ञान की संज्ञा ले रहा है कि विकास की एकतरफा खोज मानव कल्याण के लिए अहितकर हो सकती है। इसे दो अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों- समानता और स्थिरता से संतुलित किया जाना चाहिए।
इस वैचारिक जाल में फंसना आसान है कि इन लक्ष्यों की खोज में तीखे समझौते करने पड़ते हैं और संतुलन बनाना मुश्किल होता है। अल्पावधि में यह बात प्रथम दृष्टया सच है- आय के पुनर्वितरण और बाह्य प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उच्च कराधान निवेश और विकास को कम कर देंगे। फिर भी, अगर हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं, तो बहुत ही अलग निष्कर्ष सामने आ सकता है। संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षति पर ध्यान न देने वाली बेलगाम वृद्धि ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी (डायमंड 1995)। पर्यावरणीय वितरण सम्बन्धी परिणामों को कम करने की दिशा में कुछ न करने वाले पर्यावरण विनियमन से राजनीतिक प्रतिरोध और गैर-अनुपालन उत्पन्न होगा (गायकवाड़ एवं अन्य 2022)। गरीबी और असमानता को कम करने के लिए सरकारी संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें विकास द्वारा बढ़ावा मिलता है। इन पूरकताओं का लाभ उठाना ही कुँजी है।
कठिन विकल्पों से ज़्यादा, हमें दूरदर्शी विकल्प चुनने की ज़रूरत है। प्रौद्योगिकीय समाधानों (फोर्टिफाइड अनाज, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा) और मितव्ययी नीतिगत साधनों (कार्बन कर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। विकास-केन्द्रित नीतिगत ढाँचे में सिर्फ़ कुछ 'स्मार्ट नीतियों' को जोड़ना एक भूल होगी। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने और अपनी पर्यावरण नीति, सामाजिक सुरक्षा जाल और व्यापक आर्थिक प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है। अदूरदर्शी और टुकड़ों में बंटे दृष्टिकोण से एक उलझन भरी गड़बड़ी या ऐसे उपायों का एक समूह बनने का जोखिम है जो अक्सर एक-दूसरे के विरोधी काम करते हैं। मैं अपनी बात को एक या दो उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा।
प्रदूषण की धुन्ध
तेज़ी से बढ़ते भारत में शहरीकरण भी तेज़ी से हो रहा है। इसने शहरी समस्याओं का एक बड़ा ढेर ला कर खड़ा कर दिया है- हद से ज़्यादा किराया, ट्रैफ़िक जाम, चरमराता हुआ बुनियादी ढाँचा और इन सबसे बढ़कर, वायु प्रदूषण का असाधारण स्तर। सर्दियों में दिल्ली को घेरने वाले ज़हरीले धुएं के कई स्रोत हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख स्रोत दूर ग्रामीण इलाकों में स्थित है। पंजाब और हरियाणा के किसान नवंबर में गेहूँ की बुआई के लिए अपने खेत तैयार करने के लिए धान की पराली को जलाते हैं, जिससे समूचे सिन्धु-गंगा मैदान में ज़हरीला धुआं फैल जाता है।
विडंबना यह है कि फसल जलाने की पहेली का पता पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए नेक इरादों वाले कदमों से लगाया जा सकता है। ये दोनों राज्य हरित क्रांति के केन्द्र स्थल हैं, जिसने उन्हें भारत के अन्न भंडार में बदल दिया है। हालांकि, बढ़ती कृषि उत्पादकता की दर का मुकाबला औद्योगिक विकास दर नहीं कर पाई कि जिससे अतिरिक्त उपलब्ध श्रम का सही उपयोग हो पाता। व्यापार की शर्तों और कृषि आय पर पड़ रहे नकारात्मक दबाव से निपटने के लिए, सरकार ने नीतिगत साधन के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अधिक से अधिक सहारा लिया है।
हालांकि कागज़ों पर एमएसपी की पेशकश 23 फसलों के लिए की गई है, लेकिन राजकोषीय स्थान और खरीद के बुनियादी ढाँचे की सीमाओं के कारण यह मुख्य रूप से धान और गेहूँ तक ही सीमित है। फसल मिश्रण में परिणामी यह विकृति एक ओर दालों, फलों और सब्जियों की आपूर्ति में कमी, तो दूसरी ओर के बढ़ते अनाज के अतिरिक्त उत्पादन के रूप में एक साथ परिलक्षित होती है (ड्रेज़ और ओल्डिगेस 2024, आनंद 2023)। यह भारत के कुपोषण की समस्या में योगदान देने वाले असंतुलित आहार के पीछे का एक कारक हो सकता है (थॉमस 2023)। पर्यावरण के मोर्चे पर, एमएसपी और इनपुट सब्सिडी के माध्यम से पानी की अधिक खपत वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने से उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भूजल स्तर में खतरनाक गिरावट आई है।
बदले में राज्य सरकारों ने भूजल संकट से निपटने के लिए, धान की फसल के रोपण में एक वैधानिक देरी लागू की, जिससे धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच बहुत कम समय बचा। इसने शरद ऋतु के अंत में फसल अवशेषों को जल्दबाज़ी में जलाने में योगदान दिया है। इस प्रकार, आय से लेकर पानी और हवा तक का संकट फैल गया। हम समस्याओं और समाधानों के ऐसे सिलसिलों से होकर गुज़रे हैं, जिसमें प्रत्येक समाधान अपने साथ नई समस्याएं लेकर आया है।
कोई जल्दबाज़ी में एमएसपी को वापस लेने या फसल जलाने पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर सकता है, लेकिन ऐसा करना किसी अवांछित वस्तु के साथ-साथ किसी मूल्यवान वस्तु को त्यागने जैसा होगा। यह देखते हुए कि लगभग आधे भारतीय परिवार अभी भी कृषि पर निर्भर हैं, ग्रामीण-शहरी आय अंतर को नियंत्रित रखने के लिए कुछ नीतिगत हस्तक्षेप सामाजिक रूप से न्यायसंगत और राजनीतिक रूप से समीचीन दोनों हैं, जैसा कि हाल ही में किसानों के विरोध प्रदर्शनों ने इंगित किया है। समानता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ विकल्प खोजे जाने चाहिए और कुछ ऐसे प्रस्तावित भी हैं। हालांकि मैं यहाँ उनकी चर्चा नहीं करूँगा।
कई प्रौद्योगिकीय समाधान भी मौजूद हैं- उदाहरण के लिए हैप्पी सीडर मशीन (लिस्टमैन 2020 देखें) को लीजिए। जब तक सरकार सब्सिडी, विस्तार सेवाओं और सूचना प्रसार को साथ लेकर कदम नहीं उठाती, तब तक किसानों के पास इस तकनीक को अपनाने की कोई व्यक्तिगत प्रेरणा नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि किसानों को हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय 18 अरब रुपये (गुप्ता और सोमनाथन 2017) के बराबर है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के प्रत्येक निवासी पर लगभग 600 रुपये का एकमुश्त व्यय आता है, तथा सर्दियों में ठंड की मार झेलने वाले उत्तर भारतीय राज्यों के लोगों के लिए यह व्यय 35 रुपये प्रति व्यक्ति बैठता है। सभी हितधारकों के बीच लागत को समान रूप से वितरित करने वाला ‘कोएशियन समाधान’ इसका एक आसान विकल्प प्रतीत होता है, लेकिन यह एक असफल समाधान रहा है।
राजस्व से समृद्ध दिल्ली सरकार, जिसका लगभग 7 अरब रुपये का पर्यावरण कोष है और जिसे खर्च करने के लिए वह संघर्ष कर रही है। इतना पैसा कर्ज़ में डूबी पंजाब सरकार के पास नहीं पहुँच पाता है ताकि वह समस्या का मूल से ही समाधान कर सके। वित्तीय अधिकार क्षेत्र, प्रशासनिक कठोरता और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसके आड़े आती है। यहाँ तक कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की बिक्री पर लगाए गए शुल्क के माध्यम से एकत्रित, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के फंड का 80% हिस्सा भी खर्च नहीं हो पाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम ज़रूरत के मुताबिक धन का उपयोग इधर-उधर करने में असमर्थ हैं, हम धन को इधर-उधर ले जाने में असमर्थ हैं, जबकि प्रदूषक राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान किए बिना, हवा और पानी के सहारे मस्ती से फैलते जाते हैं।
1990 के दशक के उत्तरार्ध में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई गम्भीर रूप से प्रदूषित भारतीय शहरों को सार्वजनिक वाहनों (बसों, टैक्सियों और तिपहिया वाहनों) के पेट्रोल-चालित बेड़े को प्राकृतिक गैस (एलपीजी- तरल पेट्रोलियम गैस) या सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) में बदलने का आदेश दिया था। वर्ष 2010 में कोलकाता में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश परिवहन ऑपरेटरों की ईंधन प्रतिस्थापन की लागत, ईंधन लागत में बचत और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से पूरी नहीं हो रही थी (घोष और सोमनाथन 2013)। यह तथ्य विरोध प्रदर्शनों, लम्बी मुकदमेबाज़ी और इसे लागू करने में लगभग एक दशक की देरी के पीछे के कारण की व्याख्या करता है। निजी वाहनों पर मामूली कर द्वारा से एकत्रित और वित्तपोषित थोड़ी ज़्यादा सब्सिडी से कीमती समय बचाया जा सकता था।
वायु प्रदूषण के खिलाफ भारत की लड़ाई राजकोषीय रचनात्मकता की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे अनाड़ी जनादेशों की कहानी है। तकनीकी समाधान परिवर्तन की लागत को अक्सर छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से संगठित समूहों पर केन्द्रित करते हैं। विजेताओं से हारने वालों को क्षतिपूर्ति दिलाने के तरीकों के बारे में कोई विचार न होने, लाभ और हानि के बारे में विश्वसनीय आँकड़ों के अभाव तथा वोट बैंक के नुकसान के डर से सरकारें निष्क्रिय हो गई हैं। न्यायालयों ने उनकी जगह ले ली है और भारत की पर्यावरण नीति का एक बड़ा हिस्सा अब न्यायिक सक्रियता द्वारा संचालित किया जा रहा है। लेकिन, न्यायाधीशों की राजनीतिक जवाबदेही नहीं होती और न ही उनके पास पीड़ा के समान वितरण का या समाधान के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक साधन उपलब्ध होते हैं। क्या अब भी असली सरकार नहीं जागेगी?
एक समेकित पर्यावरण कोष?
वायु और जल प्रदूषण के मामले में केन्द्र और राज्य सरकारें भले ही पीछे हट गई हों पर भारत ने हाल ही में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर एक सक्रिय रुख अपनाया है, जिससे स्थानीय पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा की गई साहसिक सीओपी26 प्रतिज्ञाएँ अपने साथ जलवायु वित्त सम्बन्धी कड़ी चुनौतियाँ लेकर आई हैं। अधिकांश रूप में कोयले पर निर्भर भारतीय बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा अभी भी नगण्य है ; देश की छतों की सौर ऊर्जा की क्षमता अभी भी लगभग अप्रयुक्त है ; देश के वाहन बेड़े पुराने होते जा रहे हैं और उनमें से अधिकतर जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर हैं। हमें बदलाव करने के लिए बड़े निवेश और लक्षित सब्सिडी की आवश्यकता है।
यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे अच्छी स्थिति में भी, भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण काफी अनुकूलन लागत का सामना करना पड़ेगा (गुप्ता 2022)। मौसम की चरम घटनाएँ, मानव विस्थापन, गर्मी का तनाव, फसलों की पैदावार और उत्पादकता में कमी होगी। इस नुकसान को कम करने के लिए धन की आवश्यकता होगी और चूंकि ऐसी घटनाएँ समय के साथ बढ़ने की संभावना है, इसलिए समस्याएं विकराल होने से पहले वित्तीय लचीलापन बनाए जाने में ही समझदारी है।
जैसे कि पहले चर्चा की गई है, धन अक्सर मौजूद होता है, लेकिन अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में निहित होता है। अब समय आ गया है कि समूचे भारत के लिए एक समेकित हरित निधि बनाई जाए, जिसका प्रशासन एक ही प्राधिकरण के पास हो और जिसकी भावना जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधार की भावना के समान हो। इस बात का आकलन मुश्किल है कि जलवायु से सम्बंधित ज़रूरतें कब और कहाँ से उत्पन्न होंगी। इसलिए, हमें एक मज़बूत प्रणाली की आवश्यकता है जो संसाधनों को तेज़ी से और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में सक्षम हो।
आखिरकार, हम एक ही डूबती हुई नाव के सवार जो ठहरे।
[यह लेख मूल रूप में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में ‘भारत सतत विकास सम्मेलन’ के एक भाग के रूप में आईजीसी ब्लॉग के सहयोग से प्रकाशित हुआ था।]
अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।
लेखक परिचय : परीक्षित घोष आइडियाज़ फॉर इंडिया के प्रधान सम्पादक हैं। परीक्षित घोष दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी पीएचडी प्राप्त की है और टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में पढ़ाया है।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।




 06 जून, 2024
06 जून, 2024 


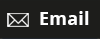

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.