भारत में कम-कुशल श्रमिकों की प्रचुरता के बावजूद, श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में उस तरह की तेज़ी कभी नहीं देखी गई जैसी समान आय स्तर वाले अन्य देशों में देखी गई है। इस लेख में तर्क दिया गया है कि इसका एक प्रमुख कारण विनिर्माण कंपनियों के सामने आने वाली संस्थागत निकास (परिसमापन) बाधाएँ हैं। लेख में देश में व्याप्त संस्थागत व्यवस्थाओं में भिन्नता का अध्ययन करते हुए पता चलता है कि ऐसी बाधाओं से न केवल ख़राब कंपनियों के निकास (परिसमापन) की गति धीमी हो जाती है, बल्कि नई कंपनियों का प्रवेश भी रुकता है, अनुत्पादक फर्में चलती रहती हैं और समग्र उत्पादन और उत्पादकता कम हो जाती है।
इस साल की शुरुआत में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया- उसने एक स्टील कंपनी के परिसमापन को रद्द कर दिया, जो चार साल पहले पूरा हो चुका था। इस फैसले ने उद्योग जगत में खलबली मचा दी, न केवल इसलिए कि इसने एक लम्बे समय से तय सौदे को उलट दिया, बल्कि इसलिए भी कि इसने इस बात की कड़ी याद दिला दी कि भारत में किसी व्यवसाय से बाहर निकलने की प्रक्रिया कितनी अनिश्चित और महंगी हो सकती है। ख़ासकर विनिर्माण क्षेत्र में लम्बा दिवाला समाधान, बोझिल प्रशासनिक मंज़ूरियाँ और सख्त श्रम कानून श्रम समायोजन और परिचालन बंद करने की लागत बढ़ा देते हैं।
ये घर्षण एक व्यापक संस्थागत परिवेश का हिस्सा हैं जिसने भारत के असामान्य संरचनात्मक परिवर्तन को आकार दिया है (फैन एवं अन्य 2021, रोड्रिक 2016)। भारत में कम-कुशल श्रमिकों की प्रचुरता होने के बावजूद, श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में उस तरह की तेज़ी कभी नहीं देखी गई जैसी समान आय स्तर वाले अन्य देशों में देखी गई है (चटर्जी और सुब्रमण्यन 2020)। बजाय इसके, विनिर्माण क्षेत्र में अकुशल कंपनियों की भरमार, पूर्णकालिक नौकरियों का सृजन और अप्रत्याशित रूप से पूँजी-प्रधान उत्पादन तकनीकों का बोलबाला रहा है (हसीह और क्लेनो 2009, पद्मकुमार 2023)।
अन्य क्षेत्रों में भारत की सफलता की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र का कमज़ोर प्रदर्शन और भी अधिक हैरान करने वाला हो जाता है। देश ने सॉफ्टवेयर निर्यात जैसे उच्च-कौशल सेवाओं में अपने निम्न औसत शिक्षा स्तर के बावजूद, आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) और आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) जैसे विशिष्ट संस्थानों की उपस्थिति के कारण उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
हम अपने नए शोध (चटर्जी एवं अन्य 2025) में यह तर्क देते हैं कि इस पैटर्न का एक मुख्य कारण विनिर्माण कंपनियों के सामने आने वाली संस्थागत निकास (परिसमापन) संबंधी बाधाएँ हैं। हम दर्शाते हैं कि ऐसी बाधाएँ न केवल कंपनियों के निकास को धीमा करती हैं, बल्कि नई कंपनियों के प्रवेश को भी रोकती हैं, अनुत्पादक कंपनियों को जीवित रखती हैं और विनिर्माण क्षेत्र में समग्र उत्पादन और उत्पादकता को कम करती हैं। इनका प्रभाव उच्च संस्थागत घर्षण वाले राज्यों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट है, जहाँ कठोर श्रम समायोजन फर्म के विकास को सीमित करता है। हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि निकास लागत को कम करने के लिए सुनियोजित ढंग से किये गए सुधार उत्पादकता, उत्पादन और रोज़गार में बड़ी वृद्धि ला सकते हैं।
भारत में कंपनियों के लिए परिसमापन इतना कठिन क्यों है?
भारत में ख़ासकर औपचारिक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र से बाहर निकलने की दरें दुनिया में सबसे कम हैं। आकृति-1 में दर्शाया है कि जहाँ अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक परिसमापन दर लगभग 9% है, वहीं भारतीय औपचारिक विनिर्माण में यह दर केवल 3.1% है। इस निम्न स्तर की गति के चलते, विशेष रूप से औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में, निकास परिसमापन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घर्षण का संकेत मिलता है, जो अधिक उत्पादक कंपनियों के लिए संसाधनों के पुनर्आबंटन को धीमा कर सकता है।
आकृति-1. चयनित देशों और क्षेत्रों में कंपनियों में परिसमापन दरें

टिप्पणियाँ/स्रोत : (i) बायाँ पैनल : विभिन्न देशों की परिसमापन दरों की गणना/निम्नलिखित स्रोतों से ली गई है ; भारत- सर्वेक्षण वर्ष 2000-01 और वर्ष 2015-16 के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण डेटासेट से परिकलित ; ब्राज़ील और मेक्सिको- बार्टेल्समैन एवं अन्य (2009) के 1990-1999 की अवधि के औसत से लिया गया ; चिली, कोलंबिया और मोरक्को- वर्ष 1985 के लिए रॉबर्ट्स और टायबाउट (1996) से लिया गया ; अमेरिका- वर्ष 2006 के लिए क्रेन एवं अन्य (2022) से लिया गया ; चीन- वर्ष 2006 के लिए वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सर्वेक्षण से परिकलित; वियतनाम - वर्ष 2007 के लिए वियतनाम उद्यम जनगणना से परिकलित। (ii) दायाँ पैनल : सेवा क्षेत्र की कंपनियों की परिसमापन दरों की गणना प्रोवेस डेटाबेस से की गई है। अन्य सेवाओं में आवास और खाद्य सेवाएँ, परिवहन और भंडारण सेवाएँ, तथा प्रशासनिक एवं सहायक सेवाएँ शामिल हैं। (iii) अनौपचारिक विनिर्माण संयंत्रों की वार्षिक परिसमापन दर की गणना वर्ष 1994-95 और वर्ष 2015-16 के एनएसएस आँकड़ों से की गई है। परिसमापन गणनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया चटर्जी एवं अन्य (2025) देखें।
संस्थागत और विनियमन संबंधी बाधाओं के कारण अनुत्पादक या संकटग्रस्त कंपनियों को बंद करना मुश्किल हो जाता है। आदर्श परिस्थितियों में भी, जब कंपनी पूरी तरह से अनुपालन करती हैं और मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होती हैं, फिर भी उसके स्वैच्छिक रूप से बंद होने में औसतन 4.3 वर्ष लगते हैं (भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21)। इनमें से लगभग तीन वर्ष आयकर कार्यालय, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) प्रशासन और भविष्य निधि प्राधिकरण जैसे सरकारी विभागों से मंज़ूरी और रिफंड प्राप्त करने में ही बीत जाते हैं। और जब बकाया ऋण, कर्मचारियों की छंटनी या कर विवाद जैसी कोई जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं तो कंपनी का बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है।
नोकिया के सबसे बड़े कारखाने का बंद होना- एक केस स्टडी
नोकिया का अपने सबसे बड़े कारखाने का अनुभव भारत में कंपनी के बाहर निकलने (बंद करने) की चुनौतियों को दर्शाता है। नोकिया ने दिसंबर 2004 में भारत में एक संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की और अंततः कर प्रोत्साहन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकटता और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी (एआईएडीएमके) और केन्द्र सरकार के बीच राजनीतिक तालमेल के कारण तमिलनाडु को चुना। वर्ष 2006 में उत्पादन शुरू हुआ। 2006 और 2012 के बीच, कारखाना खूब फला-फूला- उसने करीब 20,000 लोगों को रोज़गार दिया और 80 देशों को निर्यात के लिए मासिक डेढ़ करोड़ फोन का उत्पादन किया।
वर्ष 2013 में कारखाने के लिए मुश्किलें शुरू हो गईं- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा तेज़ हो गई, तमिलनाडु द्वारा प्रदान की गई कर छूट समाप्त हो गई, जिसके चलते विदेशी स्थान अधिक आकर्षक हो गए, सेलफोन तकनीक स्मार्टफ़ोन की ओर बढ़ने लगी थी और बेहतर रोज़गार शर्तों की मांग को लेकर श्रमिक हड़तालों का सामना करना पड़ा। नोकिया को कर चोरी के दो मामलों का भी सामना करना पड़ा- एक राज्य प्राधिकरणों से और दूसरा केन्द्रीय प्राधिकरणों से। केन्द्रीय कर विवाद के कारण अक्टूबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने नोकिया की संपत्ति ज़ब्त कर ली। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, जब नोकिया ने अप्रैल 2014 में अपना वैश्विक उपकरण और सेवा व्यवसाय माइक्रोसॉफ्ट को 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा, तो कानूनी चुनौतियों के कारण भारत में स्थापित कारखाने को इस सौदे से बाहर रखा गया। उत्पादन बंद हो गया, लेकिन उन्हें कर विवाद के दौरान स्थाई कर्मचारियों को भुगतान जारी रखना आवश्यक था। कुछ श्रमिकों ने कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विच्छेद भुगतान पैकेज स्वीकार कर लिया।
नोकिया ने वर्ष 2018 में 202 मिलियन यूरो का जुर्माना भरकर कर विवाद सुलझा लिया था, लेकिन उत्पादन बंद होने के चार साल बाद भी, यह अनिश्चित बना रहा कि क्या वह अपनी फैक्ट्री बेच पाएगा, क्योंकि बीच के वर्षों में कई अन्य मुकदमेबाजी भी हुई थीं। आखिरकार, वर्ष 2020 में, छह साल के अंतराल के बाद, चीनी कंपनी सैलकॉम्प ने उस फैक्ट्री को खरीद लिया और उसमें सेल फोन चार्जर बनाना शुरू कर दिया, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा उत्पादक सेलफोन फैक्ट्री थी।
यह उदाहरण भारत में निकास संबंधी बाधाओं के बारे में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाता है। पहला, कंपनी के निकास से जुड़ी राजनीतिक, न्यायिक और संस्थागत जटिलताएँ और अनिश्चितताएँ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होने वाली भारी देरी को दर्शाता है। तीसरा, यह अपेक्षाकृत व्यापार-अनुकूल राज्य- तमिलनाडु में हुआ, जिससे पता चलता है कि अधिक प्रतिबंधात्मक संस्थानों वाले राज्यों में निकास बाधाएँ और भी बदतर हो सकती हैं।
कंपनी के निकास को बाधित करने वाली संस्थाएँ
भारत में कंपनी के परिसमापन की बात करें तो दो मुख्य संस्थागत बाधाएँ सामने आती हैं- दिवालियापन कानून और श्रम नियम।
पहला, भारत में दिवालियापन के संदर्भ में एक सुस्पष्ट ढाँचे का अभाव है। हाल तक, दिवालियापन का सामना कर रही कंपनियों के पास परिसमापन का कोई स्पष्ट कानूनी रास्ता नहीं था, क्योंकि ये प्रक्रियाएँ कई कानूनों, जैसे कि कंपनी अधिनियम 1956 और रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 में फैली हुई थीं। इससे अनिश्चितताएँ पैदा हुईं– अलग-अलग पक्ष अलग-अलग कानूनों के तहत मामले दायर कर सकते थे और किसी कंपनी द्वारा ऋण चूक होने पर ऋण चुकाने के क्रम जैसे मुद्दों पर कोई स्पष्टता नहीं थी। परिणामस्वरूप, न्यायिक अड़चनों और कानूनों की असंगत व्याख्या के कारण विवाद अक्सर अदालतों में पहुँच जाते थे और वर्षों तक अनसुलझे रह जाते थे। इसके अलावा, अंतिम प्रतीत होने वाले निर्णयों को भी बाद में पलट दिया जा सकता था, जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक पूर्ण स्टील कंपनी के परिसमापन मामले को बदलने से स्पष्ट होता है। 1990 के दशक के आरंभ से, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई), तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जैसे विभिन्न सुधारों के प्रयास किए गए हैं, लेकिन उन्हें सीमित सफलता मिली है।
दूसरा, श्रम कानून, विशेष रूप से 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए), जिसके तहत 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन इस कानून का कार्यान्वयन अत्यधिक विवेकाधीन है। संबंधित अधिकारी या अदालत के आधार पर समान मामलों में अलग-अलग निर्णय लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अदालतें बुनियादी सवालों पर अपने फैसलों में झिझकती रही हैं, जैसे कि किन श्रमिकों और उद्योगों को श्रम कानूनों के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्या ठेका श्रमिकों को इन कानूनों के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए, इत्यादि। यह अनिश्चितता एक ऐसा माहौल बनाती है जहाँ कंपनियों, ख़ासकर वो जिनमें कई कर्मचारी होते हैं, उनके लिए निकास लागत अधिक हो जाती है।
राज्यों में निकास बाधाएँ अलग-अलग हैं और इस तरह फर्म की गतिशीलता भी अलग-अलग होती है
भारत के राज्यों में संस्थागत परिवेश में व्यापक अंतर है और इसी तरह कंपनियों के निकास की बाधाएँ भी अलग-अलग हैं। कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत व्यवसाय-अनुकूल परिवेश हैं जबकि अन्य में कठोर संस्थाएँ हैं जो परिसमापन को मुश्किल बनाती हैं। हम इस भिन्नता का उपयोग करके कई तथ्यों को दर्ज करते हैं कि विनिर्माण कंपनियाँ विभिन्न संस्थागत परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देती हैं।
सबसे पहले, राज्य स्तर पर प्रवेश और निकास सकारात्मक रूप से सह-संबद्ध होते हैं (आकृति-2 देखें- चटर्जी एवं अन्य, 2025 से पुन: प्रस्तुत)। यह स्पष्ट है कि कंपनियों के उच्च प्रवेश हिस्सेदारी वाले राज्यों में उच्च निकास हिस्सेदारी भी होती है, जो उनकी अधिक गतिशीलता को दर्शाती है। इसके विपरीत, सुस्त प्रवेश वाले राज्यों में आम तौर पर कम निकास भी देखे जाते हैं। यह पैटर्न दर्शाता है कि जहाँ निकास महंगा या अनिश्चित है, वहाँ संभावित प्रवेशकर्ता कंपनियाँ इस संभावना से हतोत्साहित हो सकती हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो वे बंद नहीं कर पाएंगी। इस पैटर्न के आधार पर, हम राज्यों को उच्च-प्रदर्शन (एचपी) और निम्न-प्रदर्शन (एलपी) श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं- एचपी राज्यों (आकृति-2 में लाल रंग से चिह्नित) में प्रवेश और निकास की हिस्सेदारी अधिक है, जबकि एलपी राज्यों (आकृति-2 में नीले रंग से चिह्नित) में दोनों की कम हिस्सेदारी है।
आकृति-2. राज्यों के कंपनियों के प्रवेश बनाम कंपनियों के निकास (परिसमापन) की हिस्सेदारी
दूसरा, गलत आवंटन, झटकों के प्रति कंपनियों की प्रतिक्रिया, और दिवालियापन सुधार के प्रभाव एचपी और एलपी राज्यों के बीच भिन्न होते हैं। एलपी राज्यों में संसाधनों का गलत आवंटन अधिक है और पुरानी और कम उत्पादक कंपनियों की एक लम्बी कतार है, जो अकुशल अस्तित्व का संकेत देती है। एलपी राज्यों की कंपनियाँ ख़ासकर जब बात अपने नियमित कर्मचारियों को समायोजित करने की हो, तो नकारात्मक झटकों के प्रति भी कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। जब वर्ष 2002 में एसएआरएफएईएसआई अधिनियम से लेनदारों के अधिकारों को मजबूत किया गया, तो इससे एलपी राज्यों में अत्यधिक ऋणग्रस्त और संकटग्रस्त कंपनियों के निकास की दर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। ये पैटर्न दर्शाते हैं कि एलपी राज्यों में निकास घर्षण अधिक बाध्यकारी हैं।
कुल मिलाकर, इन तथ्यों से पता चलता है कि जिन राज्यों में संस्थाएं कंपनियों का निकास कठिन बना देती हैं, वहाँ गलत आवंटन अधिक होता है, नई कंपनियाँ प्रवेश करने से हतोत्साहित हो सकती हैं तथा अकुशल कंपनियाँ अपेक्षा से अधिक समय तक काम करती रहती हैं।
कंपनियों के व्यवहार और नीतिगत समझौतों का मॉडल बनाना
हम कंपनियों के परिसमापन संबंधी बाधाओं के परिणामों को समझने और संभावित सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए, एक गतिशील संरचनात्मक मॉडल विकसित करते हैं जिसमें भारत के विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ शामिल हैं। इस मॉडल में शामिल कंपनियाँ ‘प्रत्याशित रूप से समान’ होती हैं, लेकिन उत्पादकता में ‘कार्योत्तर भिन्न’ हो जाती हैं, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत काम करती हैं और उन्हें डूबी हुई प्रवेश लागतों का सामना करना पड़ता है।
ख़ासकर आईडीए द्वारा कवर की जाने वाली बड़ी कंपनियों के लिए, छंटनी की लागत के कारण या न्यायिक देरी जैसे प्रत्यक्ष संस्थागत टकरावों और दिवालियापन प्रक्रिया की अनुपस्थिति के कारण निकास (परिसमापन) महंगा हो जाता है। हम इन निकास (परिसमापन) संबंधी बाधाओं का मॉडल लचीले ढंग से बनाते हैं ताकि कानून के मूल में निहित लागतों और विवेकाधीन कार्यान्वयन से उत्पन्न अनिश्चितता, दोनों को प्रतिबिंबित किया जा सके। हम एचपी और एलपी राज्यों के बीच अंतर करके संस्थागत गुणवत्ता में राज्य-स्तरीय भिन्नता को भी दर्शाते हैं। पैरामीटर अनुमान से इस बात की पुष्टि होती है कि एलपी राज्यों में निकास लागत और श्रमिक बर्खास्तगी लागत मात्रात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो पहले के वर्णनात्मक साक्ष्य के अनुरूप है। एलपी राज्यों में निकास लागत औसत वार्षिक फर्म बिक्री का 173% है, जबकि एचपी राज्यों में यह 111% है। एलपी राज्यों में नियमित कर्मचारियों की बर्खास्तगी लागत उनके औसत वार्षिक वेतन का 358% है, जबकि एचपी राज्यों में यह 256% है।
हम अनुमानित मॉडल का उपयोग ऐसे प्रतितथ्यात्मक सुधारों का अनुकरण करने के लिए करते हैं जो भारत की कंपनी की निकासी दर को अमेरिका के स्तर के 50% तक बढ़ा देंगे। इस लक्ष्य को श्रम बाज़ार में सुधार (नौकरी से बर्खास्तगी की लागत कम करना) या प्रत्यक्ष निकास (परिसमापन) को कम करके (उदाहरण के लिए, दिवालियापन का एक सुनियोजित मार्ग अपनाकर) प्राप्त किया जा सकता है।
हमारे परिणामों से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पहला- कर्मचारियों की बर्खास्तगी की लागत कम करके निकास दर बढ़ाने से मूल्य-वर्धन में 16.4% की वृद्धि होती है, लेकिन रोज़गार में 14.6% की कमी आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी, अनुत्पादक कंपनियाँ, जो पहले उच्च निकास लागत से विवश थीं, इस सुधार के बाद बाहर निकल जाएँगी। यद्यपि इससे अधिक कंपनियों को बाज़ार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन प्रवेश करने वाली कंपनियाँ, बाहर निकलने वाली बड़ी कंपनियों द्वारा विस्थापित श्रमिकों को पूरी तरह से अपने यहाँ नहीं रख पाती हैं। केवल प्रत्यक्ष निकासी लागत को कम करके निकास की दर बढ़ाने से कम रोज़गार स्तर वाली कम-उत्पादक कंपनियों की निकासी सुगम होती है और अधिक कंपनियों को बाज़ार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा नई कंपनियों द्वारा नियुक्तियाँ बाहर निकलने वाली कंपनियों से होने वाले रोज़गार नुकसान की भरपाई से कहीं अधिक होती हैं। परिणामस्वरूप, मूल्य-वर्धन और रोज़गार दोनों में क्रमशः 14.3% और 8.1% की वृद्धि होती है, जिससे यह दृष्टिकोण राजनीतिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो जाता है।
दूसरा- पूँजी आपूर्ति को अधिक लचीला बनाना (उदाहरण के लिए, विदेशी निवेश के माध्यम से) किसी भी सुधार से होने वाले लाभों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देता है। जब पूँजी आपूर्ति में अधिक लचीलापन होता है, तो किसी भी सुधार के बाद कंपनियों का प्रवेश पूँजी की उपलब्धता से कम बाधित होता है, जिससे कार्यरत कंपनियों की संख्या, मूल्य-वर्धन और रोज़गार में काफी अधिक वृद्धि होती है।
तीसरा- दोनों नीतियों के बीच मज़बूत तालमेल है। जब श्रम और निकास संबंधी सुधारों को एक साथ लागू किया जाता है, तो श्रम सुधार से होने वाले रोज़गार नुकसान कम हो जाते हैं या उलट भी जाते हैं। इससे पता चलता है कि अनुक्रमण मायने रखता है - श्रम कानूनों में सुधार से पहले प्रत्यक्ष निकास लागत (दिवालियापन कानून में सुधार के माध्यम से) से निपटने से दक्षता में सुधार करते हुए नौकरियों को संरक्षित करने में मदद मिलती है।
हम प्रवेश को बढ़ावा देने और निकास को सुगम बनाने के बीच सुधार बजट आवंटित करने के परिणामों की भी जाँच करते हैं। विकासशील देशों में सरकारें अक्सर कर छूट, औद्योगिक पार्कों और स्टार्टअप सब्सिडी के माध्यम से नई कंपनियों के प्रवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्रवेश बाधाओं को कम करने से वास्तव में उत्पादकता और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है (ब्रांट एवं अन्य 2024, सैम्पी एवं अन्य 2023)।
हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि किसी दिए गए बजट के लिए, निकास (परिसमापन) लागत कम करने से ख़ासकर उच्च बजट स्तरों पर मूल्य-वर्धित लाभ में कहीं अधिक वृद्धि होती है। यदि उद्देश्य मूल्य-वर्धित लाभ को अधिकतम करना है, तो निकास लागत को लक्षित करना अधिक प्रभावी है। यदि लक्ष्य रोज़गार को बढ़ावा देना है, तो नई कंपनियों के प्रवेश के लिए सब्सिडी बेहतर परिणाम देगी।
अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।
लेखक परिचय : शौमित्रो चटर्जी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफ़ेसर हैं। उनकी शोध रुचियाँ विकास अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्संबंध पर केंद्रित हैं और उनके शोध का एक पहलू कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यापार और बाज़ार शक्ति पर केंद्रित है जबकि दूसरा पहलू वैश्वीकरण, विकास और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित है। वे सेंटर फ़ॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के एक शोध सहयोगी और पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के सेंटर फ़ॉर एडवांस्ड स्टडी ऑफ़ इंडिया में एक गैर-आवासीय फ़ेलो भी हैं। वे पेन्सिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में संकाय सदस्य रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2015-16 के दौरान भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 2018 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 2018-19 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आईइनईटी-पोस्टडॉक्टरेट रहे हैं। वर्ष 2024 में द प्रिंट द्वारा उन्हें अगले दशक के भारत के आर्थिक विचारकों में से एक के रूप में नामित किया गया। कला कृष्णा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की लिबरल आर्ट्स रिसर्च प्रोफ़ेसर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए और एमए करने के बाद, उन्होंने 1984 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे 1984-1992 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की सहायक और एसोसिएट प्रोफ़ेसर, 1992-1993 तक टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल ऑफ़ लॉ एंड डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों की विलियम एल क्लेटन प्रोफ़ेसर और 1993 से पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफ़ेसर रहीं। उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, द रिव्यू ऑफ़ इकोनॉमिक स्टडीज़, द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिव्यू, द अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल्स, द जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आदि में लेख प्रकाशित किए हैं। उन्होंने विश्व बैंक और आईएमएफ के लिए परामर्शदात्री के रूप में कार्य किया है। उनकी शोध रुचियाँ व्यापार, विकास, औद्योगिक संगठन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नीलामी, अपराध और हाल ही में शिक्षा में हैं। उन्होंने स्वैच्छिक निर्यात प्रतिबंध, मुक्त व्यापार क्षेत्र और उत्पत्ति के नियम, और मल्टी फाइबर व्यवस्था सहित व्यापार नीति के मुद्दों पर व्यापक रूप से काम किया है। कल्याणी पद्मकुमार फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर हैं। उनकी शोध रुचियाँ विकास अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रतिच्छेदन में हैं, जहाँ उनका काम विकासशील देशों में फर्मों पर सरकारी नियमों के प्रभाव को मापने पर केंद्रित है, जिसमें न्यून-रूप और संरचनात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने जुलाई 2023 में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। यिंग्येन ज़ाओ जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय और इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर हैं। उनका शोध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है, और हाल की परियोजनाएँ व्यापार में टकराव के बारे में हैं।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।




 18 सितंबर, 2025
18 सितंबर, 2025 


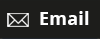





Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.