हर जून में दो महत्वपूर्ण दिन आते हैं, एक पर्यावरण से संबंधित और दूसरा बाल श्रम से संबंधित। "आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें!" 12 जून को मनाए जाने वाले बाल श्रम विरोधी दिवस की थीम के परिपेक्ष्य में यह चिंतन करने का समय है कि बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए क्या आवश्यक है। विकासशील दुनिया में बाल श्रम के विरुद्ध प्रतिबंध और विनियमन, इस समस्या को हल करने के सबसे लोकप्रिय नीतिगत उपायों में से हैं। लेकिन ये व्यवहार में कितने कारगर हैं? कई वर्ष पूर्व का यह शोध आलेख आज भी प्रासंगिक है। आलेख में बाल श्रम के विरुद्ध भारत के प्रमुख कानून,1986 के बाल श्रम अधिनियम की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इस प्रतिबंध के कुछ वर्षों बाद, 14 वर्ष की कानूनी रोज़गार आयु की तुलना में कानूनी आयु से कम आयु के बच्चों के रोज़गार स्तर में वृद्धि हुई।
दशकों से लगभग सार्वभौमिक विरोध का सामना करने के बावजूद, बाल श्रम स्थानिक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की पिछले दशक की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 16 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक मौजूद थे, जिनमें से 8 करोड़ 50 लाख खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे (आईएलओ 2013)।
इस समस्या से निपटने के लिए कई नीतिगत विकल्प मौजूद हैं, उनमें बाल श्रम के खिलाफ प्रतिबंध और विनियमन दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय नीतिगत उपायों में से हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कानून हमेशा बाल श्रम में कमी लाएंगे। यदि इन्हें पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो ये प्रतिबंध नियोक्ताओं को बाल श्रम के उपयोग को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। वास्तव में, जिन देशों में बाल श्रम प्रचलित है, उनकी सरकारों के पास शायद ही कभी बाल रोज़गार पर विनियमन को पूरी तरह से लागू करने की क्षमता और संसाधन होते हैं, जैसा कि अर्थशास्त्रियों, एरिक एडमंड्स और महेश्वर श्रेष्ठ (2012) द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया है। जब प्रतिबंध अपूर्ण रूप से लागू होते हैं तो बच्चों को काम पर रखने की लागत बढ़ जाती हैं, क्योंकि नियोक्ता बाल श्रम का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर कठोर जुर्माना या अन्य दण्ड का सामना करने के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार, प्रतिबंध केवल बच्चों को दिए जाने वाले वेतन को कम कर सकते हैं। यदि परिवार ज़रूरतों के चलते अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं, तो बाल मज़दूरी में गिरावट से उन परिवारों की आय कम हो जाती है, जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाल श्रम पर निर्भर रहते हैं। इससे परिवारों को कम बाल श्रम कराने के बजाय अधिक बाल श्रम कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है (बसु 2005)।
प्रत्यक्ष रूप में बाल श्रम प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है
वर्ष 2007 के एक व्यापक समीक्षा लेख में, एरिक एडमंड्स ने निष्कर्ष निकाला, "...इस सारी नीतिगत चर्चा के बावजूद, काम पर प्रतिबंधों की प्रभावशीलता का कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं दिखता है जो साक्ष्य के वर्तमान मानकों को पूरा करे।" शोध साहित्य में इस महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए हम बाल श्रम के खिलाफ भारत के प्रमुख कानून, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय रोज़गार सर्वेक्षणों से प्राप्त व्यक्तिगत स्तर के डेटा का उपयोग करते हैं (भारद्वाज, लकड़ावाला और लिया 2013)। हालांकि वर्ष 1986 का अधिनियम भारत में लागू किया गया पहला बाल श्रम कानून नहीं था, लेकिन इसने एक सख्त और अधिक समान संहिता लागू की और मीडिया में इस कानून को भारत में बाल श्रम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उद्धृत किया गया है। विशेष रूप से, वर्ष 1986 के अधिनियम ने अधिकांश विनिर्माण और सेवा व्यवसायों में 13 वर्ष और उससे कम आयु के बच्चों के रोज़गार पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि घंटों के विनियमन के अधीन कृषि और पारिवारिक व्यवसायों में इन बच्चों को रोज़गार की अनुमति दी। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सम्भावित जेल की सजा का सामना करना पड़ा।
बढ़ती आय और स्कूल नामांकन के परिणामस्वरूप 18 वर्ष से कम आयु के भारतीयों के लिए समग्र रोज़गार दरें साल दर साल गिर रही हैं, जबकि हम दर्शाते हैं कि प्रतिबंध के बाद, 14 वर्ष की कानूनी कार्य-आयु से कम आयु के बच्चों के रोज़गार स्तर वास्तव में कानूनी आयु (14-17 वर्ष की आयु) के बच्चों के सापेक्ष बढ़ गए हैं। इस प्रकार वर्ष 1986 का अधिनियम, जिसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सापेक्ष रोज़गार को कम करना था, उसका कुछ हद तक विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रतिबंध के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने की सम्भावना 1.7 प्रतिशत अधिक है। यह देखते हुए कि प्रतिबंध से पहले 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 14% बच्चे कार्यरत थे, यह बाल रोज़गार में 12% की वृद्धि के बराबर है।
प्रतीत होता है कि यह प्रभाव आंशिक रूप से बच्चों के वेतन में बड़ी गिरावट से उपजा है। वर्ष 1986 के अधिनियम के मुख्य लक्ष्य रहे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वेतन बड़े बच्चों और वयस्कों के वेतन के सापेक्ष 4% कम हो गया। इस प्रकार प्रतिबंध ने, प्रतिबंध से प्रभावित क्षेत्रों में, बच्चों के रोज़गार पर कर के रूप में काम किया, एक ऐसा कर जो कम वेतन के रूप में बाल कर्मियों पर डाला गया। यह खोई हुई मज़दूरी विनिर्माण और कृषि, दोनों क्षेत्रों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सापेक्ष रोज़गार में वृद्धि के साथ मेल खाती है, लेकिन इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र में केन्द्रित है, जहाँ छोटे बच्चों का सापेक्ष वेतन अप्रभावित था। चूंकि शुरू में विनिर्माण की तुलना में कृषि में बच्चों का वेतन कम था, इसलिए कम विनिर्माण वेतन और कृषि में रोज़गार के बड़े हिस्से के संयोजन के परिणामस्वरूप, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय में 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों की आय के सापेक्ष 10% की गिरावट आई।
भारत के बाल श्रम प्रतिबंध के कारण कौन से परिवार सबसे अधिक प्रभावित हुए
चूँकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मज़दूरी में और गिरावट आई है, इसलिए उस आयु सीमा में काम करने वाले बच्चों वाले गरीब परिवारों को आय में और भी अधिक हानि हुई और हम यह मान सकते हैं कि इसका प्रभाव उन परिवारों में केन्द्रित होगा। जब हम 10-13 आयु वर्ग के भाई-बहनों वाले बच्चों- जिन पर प्रतिबंध के मज़दूरी प्रभावों के कारण पारिवारिक आय में कमी के अनुभव की सबसे अधिक सम्भावना है, पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रतिबंध के परिणामस्वरूप उन बच्चों को काम पर लगाए जाने की सम्भावना लगभग 5.6% अधिक है जिनके इस आयु वर्ग में कोई भाई-बहन नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोज़गार में वृद्धि, 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों की तुलना में सबसे गरीब परिवारों में केन्द्रित है- ऐसे परिवार जिनमें परिवार के मुखिया की शिक्षा माध्यमिक स्तर से नीचे है या वे परिवार जिनके भोजन में मुख्य रूप से सबसे सस्ती खाद्य वस्तुएं शामिल हैं।
अंत में हम ऐसे अन्य तरीकों का पता लगाते हैं जिनसे प्रतिबंध से परिवार प्रभावित होते हैं। बाल रोज़गार में हम जो वृद्धि देख रहे हैं, उसका परिणाम स्कूल में उपस्थिति में कमी के रूप में नहीं होगा यदि ये बच्चे पहले से आर्थिक रूप से 'निष्क्रिय' हों, घरेलू उत्पादन में लगे हुए हों या अवकाश का आनंद ले रहे हों। हालांकि हमारे परिणाम दर्शाते हैं कि कुछ बच्चों को काम करने के लिए वास्तव में स्कूल से निकाला जा रहा है- पहले की तुलना में 10-13 वर्ष की आयु के भाई-बहन वाले बच्चों के स्कूल जाने की सम्भावना, जिनके 10-13 वर्ष की आयु के भाई-बहन नहीं हैं, प्रतिबंध के बाद 1.4% कम है। प्रतिबंध का एक और प्रभाव बच्चों को मज़दूरी से हटाकर पारिवारिक उद्यमों में लगाना हो सकता है, जिससे 10-13 वर्ष की आयु के बच्चों वाले परिवारों की कुल पारिवारिक आय में बड़ी कमी को रोका जा सकता है, भले ही बच्चों से प्राप्त होने वाली मज़दूरी आय में कमी हो। वैकल्पिक रूप से, परिवारों ने पारिवारिक आय में इस गिरावट के जवाब में अपने व्यय में कटौती की होगी या अपनी परिसम्पत्तियों को कम किया होगा। हमने प्रति व्यक्ति व्यय, खाद्य व्यय, कैलोरी सेवन और पारिवारिक परिसम्पत्ति सम्पदा के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ़ हाउसहोल्ड एसेट वेल्थ) सहित पारिवारिक कल्याण के कई उपायों की जाँच की और पाया कि 10-13 वर्ष की आयु के बच्चों वाले परिवारों के लिए इन उपायों में थोड़ी गिरावट आई है। जो यह दर्शाता है कि गरीब परिवारों की विभिन्न मुकाबला करने की रणनीतियाँ, जिसमें बाल श्रम के लिए बढ़ा हुआ प्रावधान शामिल है, बच्चों से खोई हुई मज़दूरी आय की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त हैं।
कुल मिलाकर, हमारे परिणाम दर्शाते हैं कि 10-13 वर्ष के बच्चों वाले परिवार वर्ष 1986 के अधिनियम के बाद बच्चों की मज़दूरी में गिरावट, बाल रोज़गार में वृद्धि, बाल स्कूली शिक्षा में गिरावट, तथा पारिवारिक उपभोग और सम्पत्ति में गिरावट के सन्दर्भ में बड़े बच्चों वाले परिवारों की तुलना में बदतर स्थिति में हैं।
नीति के लिए निहितार्थ
ये परिणाम उन परिस्थितियों में बाल श्रम प्रतिबंधों के प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहाँ लोग निर्वाह के हाशिए पर रहते हैं और जहाँ कानूनी प्रवर्तन कमज़ोर है। भारत में वर्तमान नीतिगत माहौल को देखते हुए वे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें रोज़गार के अधिकार (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, मनरेगा) या शिक्षा के अधिकार जैसे कुछ अधिकारों की कानूनी गारंटी शामिल है। हालांकि ऐसी नीतियों के लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे अधिकार भ्रष्टाचार के व्यापक सन्दर्भ और गरीब परिवारों की व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं। शायद हमारे निष्कर्षों के लिए सबसे प्रासंगिक, फरवरी 2013 में भारत की संसद में एक विधेयक पेश किया गया था जिसमें सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। अन्य प्रावधानों के अलावा, प्रस्तावित विधेयक में ऐसे कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं के लिए निगरानी और दण्ड बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। हमारे शोधपत्र के परिणाम व्यापक संस्थागत और बाजार विफलताओं की उपस्थिति में ऐसी नीतियों के प्रति आगाह करते हैं। भले ही प्रस्तावित विधेयक को आक्रामक तरीके से लागू किया गया हो और वास्तव में बाल श्रम को कम करने में सफलता मिली हो- और यह सम्भव है कि पारिवारिक उद्यमों या किसी भी क्षेत्र के लिए कोई छूट न देने वाला प्रतिबंध लागू करना आसान हो- इससे प्रभावित परिवारों की आय में होने वाली गिरावट से परिवार के वयस्कों और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय में पर्याप्त गिरावट शामिल है।
हमारे निष्कर्ष बाल श्रम के विरुद्ध सरकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की नीतियों को हतोत्साहित नहीं करते हैं।1 नीति-निर्माताओं के पास जो बाल श्रम की घटनाओं को कम करना चाहते हैं, परिवारों को नकद हस्तांतरण और शिक्षा में निवेश बढ़ाना जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। हमें लगता है कि इन विकल्पों के बारे में नीतिगत विचारों में चर्चा को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हमारे अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के तहत लगाए गए बाल श्रम प्रतिबंध अप्रभावी हो सकते हैं। यह समझना कि बाल श्रम अक्सर गरीब परिवारों का अंतिम सहारा होता है, यह दृष्टिकोण गरीब परिवारों की मदद कर के बाल श्रम की आपूर्ति को कम करने पर केन्द्रित है, न कि बाल श्रम की मांग को सीमित करने पर, जिससे उनकी आय कम होगी और विकृत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
इस लेख का एक संस्करण वॉक्सईयू (www.voxeu.org) पर प्रकाशित है।
टिप्पणी:
- उत्पाद बहिष्कार का मामला नीति का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया एक उदाहरण है जिसे सरकारें विनियामक परिवर्तन लाने के लिए लागू करती हैं। हालांकि, ये भी अपेक्षा से कम प्रभावी हो सकते हैं (डोइप्के और ज़िलिबोट्टी 2010; और कई अन्य।)
अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।
लेखक परिचय : प्रशांत भारद्वाज कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। लिया के. लकड़ावाला मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। निकोलस ली टोरंटो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।




 13 जून, 2024
13 जून, 2024 


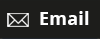



Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.