वन अधिकार अधिनियम (2006) भारत में एक ऐतिहासिक वन कानून था, जिसके तहत वन संसाधनों पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई। हालांकि नवंबर 2018 तक देश भर में प्राप्त कुल दावों में से केवल 44.83% मामलों में हीं स्वामित्व प्रदान किया गया है। सायक सिन्हा ने महाराष्ट्र में किए क्षेत्र अध्ययन के आधार पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का वर्णन किया है, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े आदिवासियों तथा वनवासियों द्वारा अधिकार प्राप्त करने को मुश्किल बनाते हैं।
वन या जंगल जटिल सामाजिक-पारिस्थितिक संरचनाएं हैं जो उनके भीतर रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हैं। वन के बाहर रहने वाले लोग इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। वनों के शासन संबंधी व्यवस्था, वनों के महत्व तथा उनके भीतर एवं बाहर रहने वालों के साथ उनके संबंधों के बारे में विभिन्न कथनों के बीच स्थित रही है। वनों की इस जटिलता के कारण ही आज तक राज्य को वनों की एक मजबूत परिभाषा तैयार करने में अक्षम रही है। इस प्रकार वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 का पारित होना भारत में वन कानून के संबंध में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग पर ‘आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदायों’ के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी थी। यह वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। दशकों तक उन्हें जंगलों से बाहर रखने और उनकी पहुंच को सीमित करने की कोशिश के बाद यह कानून वनों को लोगों को वापस सौंपना चाहता है, और वनों के संरक्षण में उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। हालाँकि इसका क्रियान्वयन बहुत सुचारू नहीं रहा है। इस कानून ने संरक्षण और क्रियान्वयन के आधार पर विवाद भी देखे हैं। नवंबर 2018 तक पूरे भारत में प्राप्त कुल दावों में से केवल 44.83% मामलों में स्वामित्व प्रदान किया गया है। इस लेख में मैंने वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के दो गांवों में किए गए प्रतिभागीयों के अवलोकन संबंधी अध्ययनों के आधार पर एफआरए के इन दो समस्या क्षेत्रों पर चर्चा की है, और इसके निष्कर्षों को एफआरए के संदर्भ में की जाने वाली बड़ी बहस के लिए रखा है।
ऐतिहासिक संदर्भ
वनों के लिए नीतियों के केंद्र और बाद की बहसों ने लगभग दो तरह के तर्क दिए हैं। पहला यह है कि आदिवासियों और अन्य वनवासी समुदायों की आजीविका के साधनों की रक्षा करने और उनके प्रति किए गए ऐतिहासिक अन्यायों की अनदेखी करना, जो परंपरागत रूप से पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर हैं। दूसरा, वन-संसाधनों का राज्य-नियंत्रित दोहन, वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण और यथासंभव व्यापक पैमाने पर मानव हस्तक्षेप से उन्हें दूर रखना। दूसरा तर्क इतिहास के अधिकांश हिस्से के लिए प्रमुख कथन रहा था। भारतीय वन अधिनियम, 1865 और उसके बाद के विधानों से शुरू होकर, औपनिवेशिक राज्य ने वन भूमि पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और पारंपरिक वनवासी समुदायों (गुहा 1983) की पहुंच को प्रतिबंधित किया। आजादी के बाद नेहरूवादी राज्य के पूरी तरह से औद्योगिकीकरण पर जोर देने के साथ-साथ वनों को सरकार के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाता रहा, और उनके आर्थिक दोहन (गुहा 1983) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
दोनों दृष्टिकोणों में वनों के शासन के संबंध में परिणामी विधान और राज्य के विरोधाभासी व्यवहार प्रतिबिंबित होते हैं। जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और वन संरक्षण अधिनियम (1980) में मनुष्यों की पहुँच को सीमित करके वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास है। वन अधिकार अधिनियम (2006) वनवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और वनों तक उनकी पहुँच को संस्थागत बनाने की आवश्यकता को मान्यता देता है। इस प्रकार, भारतीय राज्य ने वन-आश्रित लोगों की आजीविका और आश्रय के पुनर्वास के लिए वैधानिक व्यवस्था करते हुए वनों तक उनकी पहुँच को सीमित करके एक संरक्षक की भूमिका निभायी। राज्य के इस दोहरे रवैये से अधिनियम के कार्यान्वयन के दायरे में काफी हद तक अति व्याप्तता आई है। एफआरए को लागू करने का विशेषाधिकार किसी एक विभाग के पास नहीं है, लेकिन इसके लिए राजस्व, ग्रामीण विकास और वन विभागों को मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक को भूमि की उचित पहचान में शामिल होना चाहिए और वनों का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
क्षेत्र से अवलोकन
महाराष्ट्र में सांगली जिले के लेंगरे गांव में ग्रामीणों को जिला वन विभाग के साथ कानूनी लड़ाई में उलझना पड़ा। यह गाँव वन भूमि के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। वन विभाग ने दावा किया कि ग्रामीणों ने खेती के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। वर्ष 1998 में 73 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और यह मामला सात साल तक खिंचा। अंत में, फैसला ग्रामीणों के पक्ष में आया। ग्रामीणों ने बाद में एफआरए के तहत अधिकार प्राप्त करने का दावा प्रस्तुत किया। हालांकि एफआरए की प्रशासनिक संरचना के कारण उन्हें उनके अधिकारों से अगले 1.5 साल तक वंचित रखा गया था। महाराष्ट्र के सभी हिस्सों से 40,000 किसानों के मुंबई जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप किए जाने के कारण खेती के अधिकार सहित व्यक्तिगत वन अधिकारों को प्राथमिकता दी गई और इन्हें राज्य भर में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) के माध्यम से सख्ती के साथ लागू किया गया। इस अभियान के तहत, जब पुणे डिवीजन के घोड़ेगाँव के आईटीडीपी के अधिकारियों को लेंगरे की कानूनी पेचीदगियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने गाँव में एफआरए का क्रियान्वयन शुरू किया।
तब तक राजस्व, ग्रामीण विकास और वन विभाग अपने दावों को दर्ज करने में ग्रामीणों की मदद करने के लिए एक साथ नहीं आए थे। वे एक साथ केवल आईटीडीपी के हस्तक्षेप के बाद ही आए जिसने 73 किसानों की कृषि भूमि के मानचित्रण को संभव बनाया। हालांकि इन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के शुरुआती उत्साह के ठंडा पड़ जाने के बाद ग्रामीणों के लिए ग्रामीण स्तर के अधिकारियों के समक्ष अपना दावा दायर करना फिर से मुश्किल हो गया। फिर एफआरए के क्रियान्वंयन पर काम कर रहे एक एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन) आदिवासी कल्याण संवर्धन ने हस्तक्षेप किया और नौकरशाही प्रक्रियाओं को संभालने में ग्रामीणों की मदद की। एनजीओ ने आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में किसानों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि दावों को गाँव, उप-मंडल और जिला स्तरों पर समीक्षा के तीन स्तरों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया का बिल्कुल ठीक प्रकार से पूरा किया जाना आवश्यक है इसलिए एनजीओ का यह कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है कि उन्होंने दावे पारित होना सुनिश्चित किया।
हुम्बे बस्ती, पुणे जिले के भोर ब्लॉक में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक छोटी-सी बस्ती है। यह जयतपाड नामक एक बड़े गाँव का हिस्सा है जो पहाड़ी के नीचे स्थित है। इस बस्ती में कुल आठ घर हैं। हुम्बे पारंपरिक मवेशी चरवाहे हैं जो पहाड़ी के नीचे कृषि कार्य करते हैं। उनमें से कुछ लोग अंशकालिक नौकरियां करने के लिए पुणे जाते हैं, जैसे कि मालिश करने वाले, सफाई करने वाले, माली, आदि। हुम्बे लोगों का दावा है कि वे आदिवासी हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें ओटीएफडी श्रेणी (अन्य पारंपरिक वनवासी) में सूचीबद्ध किया है। यह बस्ती घने जंगलों से घिरी हुई है, और मवेशियों पर जंगली जानवरों के हमले यहां आम बात है। इस कृषि भूमि के लिए उन्होंने खेती के व्यक्तिगत वन अधिकारों का दावा किया था। ग्रामीणों ने पहले एक दावा दायर किया था जिसे निवास के प्रमाण की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। गाँव की वन अधिकार समिति को अपना दावा दायर करने के लिए गाँव वालों के पास जयतपाड की ग्राम सभा को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी। आगे जैसा कि लेंगरे मामले में हुआ था। तीनों विभागों का साथ इस तथ्य के कारण हासिल करना मुश्किल था कि गांव में सड़कों की कमी थी और इसलिए इन विभागों के ग्राम-स्तर के अधिकारियों के लिए कोई पहल करने हेतु यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पुन: आईटीडीपी की पहल के कारण ही गाँव में बैठकें हुईं, ग्रामीणों को अपने दावे दाखिल करने में मदद मिली, और तीनों क्रियान्वयन विभाग दावों को पास करने के लिए एक साथ आए।
व्यापक निहितार्थ
हजारों वर्षों से आदिवासी तथा अन्य वनवासी जंगलों में रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं और गैर-इमारती वन उत्पाद का उपभोग करते हैं। प्रत्येक क्रियान्वयन विभाग के अपने-अपने हित हैं। उदाहरण के लिए - वन विभाग का ध्यान वन भूमि की सुरक्षा और इन जमीनों को अपने सीधे नियंत्रण में रखने पर अधिक है जबकि राजस्व विभाग मुख्य रूप से कर संग्रह बढ़ाने में रुचि रखता है। ऐसे परिदृश्य में आदिवासियों को वसीयत के साथ संपर्क करने में सक्षम होने के लिए नौकरशाही बाधाओं से गुजरने, कई प्रमाणों को संकलित करने तथा उनका दस्तावेजीकरण करने, और पूरी तरह से सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना उसी प्रकार आवश्यक होता है जैसा कि कस्बों एवं गांवों के लोग करते हैं। इसके बावजूद कि वे सामाजिक और राजनीतिक रूप से बाकी नागरिकों से दूर हैं। एफआरए ने एक तरह से हाशिए के लोगों को राज्य के बहुत करीब ला दिया है और उन्हें नागरिकों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया है।
लेंगरे और हुम्बे बस्ती जैसे गांवों में लोग जटिल प्रक्रियाओं के जाल में फंस गए हैं। उन्हें राज्य-समाज के एक प्रकार के संवाद का हिस्सा होना चाहिए जिसके लिए वे न तो पर्याप्त रूप से साक्षर हैं, और न ही अनुभवी। राज्य को समाज के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि इसकी प्रकृति उन स्थानों के रहने वालों के लिए समझ में आने वाली और लाभप्रद हो, जो इन मामलों में बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि इन दो गांवों में देखा गया है, ग्रामीण इन नौकरशाही जटिलताओं में उलझ गए थे और अपनी ही जमीन पर कानूनी अधिकार प्राप्तर करने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। मामले इस तथ्य से और जटिल हो जाते हैं कि ये ऐसी भूमि हैं जहां लोग रहते हैं और कृषि कार्य करते हैं। यही वह जमीन है जो उन्हें आश्रय और आजीविका देती है और इसे प्राप्त करने के लिए सभी कानूनी बाधाओं को आसानी से दूर किया जाना चाहिए। इसलिए एफआरए में तत्काल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे लोगों के प्रति न्यायसंगत हो और उन्हें जीवन और जीवन-निर्वाह का अधिकार दे।
लेखक परिचय: सायक सिन्हा एक सार्वजनिक नीति सलाहकार (पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट) हैं।




 24 जुलाई, 2020
24 जुलाई, 2020 


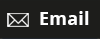

Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.