वर्ष 1973 से प्रतिवर्ष जून की 5 तारीख का विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पालन किया जाता है। पर्यावरण के सभी घटकों, पर्यावास और प्राणियों का आपसी सम्बन्ध अति सूक्ष्म और जटिल होता है, यह दिन इसी जागरूकता के प्रसार-प्रचार और कार्यवाही को समर्पित है। पर्यावरण दिवस पर प्रस्तुत इस लेख में औद्योगिक जल प्रदूषण पर चर्चा की गई है। हालांकि सभी प्रमुख भारतीय शहरों में झीलों, नदियों में नियमित रूप से ज़हरीला झाग दिखाई देता है, जल प्रदूषण पर वायु प्रदूषण जितना ध्यान नहीं दिया जाता है। औद्योगिक जल प्रदूषण के कृषि पर प्रभाव की जांच करते हुए इस लेख में दर्शाया गया है कि औद्योगिक स्थलों के नीचे की ओर की नदियों में प्रदूषक तत्वों की सांद्रता यानी सेचुरेशन में अचानक बड़ी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, फसल की पैदावार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।
कम और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में प्रदूषण का स्तर अक्सर ऊँची आय वाले देशों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खराब होता है। इसके बावजूद, प्रदूषण की लागत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसकी समझ ज़्यादातर विकसित देशों (कीज़र और शापिरो 2019, करी और वॉकर 2019) से आती है। उन निष्कर्षों को एलएमआईसी पर लागू करने का बहुत ही कम आधार मौजूद है। भारत में जल प्रदूषण को वायु प्रदूषण जितना ध्यान अब तक नहीं मिला है, भले ही यह एक बड़ा मुद्दा है। नई दिल्ली और बेंगलुरु (मूलर-गलैंड 2018) जैसे महानगरों में झीलों और नदियों पर नियमित रूप से ज़हरीला झाग तैरता हुआ दिखाई देता है। वहाँ मछलियों का मरना अब एक आम बात हो गई है (व्यास 2022)। जबकि सार्वजनिक दबाव के कारण वायु प्रदूषण के नियम काफी सख्त हो गए हैं, लेकिन इस तरह के प्रयासों से पानी की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ है (ग्रीनस्टोन और हैना 2014)।
वैसे यह बात है कि ऊँची आय वाले देशों में भी जल प्रदूषण की सामाजिक लागत पर कोई स्पष्ट मूल्य का टैग लगा पाना मुश्किल काम है। हालांकि सर्वेक्षणों के अनुसार लोग पानी की गुणवत्ता के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन शोध अध्ययन अक्सर जल प्रदूषण के बड़े आर्थिक प्रभावों को खोजने में विफल रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है लागत वास्तव में कम है, या फिर ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जल प्रदूषण का अध्ययन करना कठिन है। सीमित डेटा, जल प्रदूषण कैसे आगे बढ़ता है- इसकी मॉडलिंग की चुनौतियाँ और प्रदूषकों की विशाल संख्या ने इस प्रश्न का अध्ययन करना बड़ा कठिन बना रखा है। इस कारण से सम्भव है कि इसके वास्तविक प्रभावों का कम आंकलन हो रहा हो (कीज़र और शापिरो 2019)।
हमारा अध्ययन
अपने अध्ययन में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि औद्योगिक जल प्रदूषण भारत में कृषि उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है (हेगर्टी और तिवारी 2024)।1 कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि इसमें अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में अधिक पानी का उपयोग होता है- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के 2018 के अनुमानों के अनुसार लगभग चार गुना अधिक। और सिंचाई के पानी का कभी उपचार नहीं किया जाता है। खेती-बाड़ी लगभग हर क्षेत्र में होती है, इसलिए इसके प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से प्रभावित होने की संभावना है। हम 2009 में भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'गम्भीर रूप से प्रदूषित' घोषित 48 औद्योगिक स्थलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जगहें दुनिया के सबसे प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों (मोहन 2021) में आती हैं और यही कारण उन्हें जल प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनाता है।
जल प्रदूषण फसलों को कैसे प्रभावित करता है?
उद्योगों से निकलने वाले पानी में सभी प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, जिनमें भारी धातु, उच्च लवणता, असामान्य रूप से कम या बहुत अधिक pH वाले अपशिष्ट और विषैले कार्बनिक यौगिक शामिल होते हैं। ये अपशिष्ट पौधों के विकास को रोककर या फिर पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करके फसलों को गम्भीर नुकसान पहुँचा सकते हैं (बाजपेई 2013, सुदर्शन एट अल. 2023, स्कॉट एवं अन्य 2004)। सिंचाई के लिए प्रदूषित पानी का उपयोग करने वाले प्रयोगों के परिणामों में धान (चावल) के खराब विकास और खराब स्वाद जैसे बड़े प्रभाव सामने आए हैं (विश्व बैंक और राज्य पर्यावरण संरक्षण प्रशासन, 2007)। लेकिन ऐसे प्रयोग वास्तविक दुनिया की स्थितियों को नहीं दोहराते हैं, जहाँ स्रोत से खेतों तक पहुँचने से पहले प्रदूषण बड़े जटिल मार्गों और तरीकों से होकर आ सकता है। हमारा अध्ययन इस समस्या को सावधानीपूर्वक मॉडलिंग के ज़रिए खोजने की कोशिश करता है कि प्रदूषण फसलों तक कैसे पहुँचता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी औद्योगिक अपशिष्ट हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ अपशिष्टों में नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम जैसे उपयोगी रसायन होते हैं। ये वही तत्व हैं जो उर्वरकों में पाए जाते हैं। यदि ये रसायन कम मात्रा में होते हों तो वास्तव में फसलों को उगाने में मदद कर सकते हैं (हॉकिन्स और रिसे 2017, बिडेन और असफॉ 2023, झांग और लू 2024)। हानिकारक और सहायक प्रभावों के इस मिश्रण के कारण, फसलों पर पड़ने वाला औद्योगिक प्रदूषण का समग्र प्रभाव एक अनुभवजन्य प्रश्न है जिस पर हम अपने शोध में काम करते हैं।
अनुसंधान का डिज़ाइन
हमारा शोध डिज़ाइन जल प्रदूषण की एक प्रमुख विशेषता का उपयोग करता है- विशेषता यह है कि वायु प्रदूषण के उलट, जल प्रदूषण लगभग हमेशा अपने स्रोत से केवल एक ही दिशा में बहता है। जब उद्योग नदियों में अपना अपशिष्ट जल बहाते हैं तो प्रदूषण का स्तर नदी के बहाव के नीचे की ओर बढ़ जाता है जबकि ऊपर की ओर का जल अपेक्षाकृत अप्रभावित रहता है। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों में अन्य कोई अंतर न होने की संभावना होती है। इससे बहाव के नीचे की ओर के क्षेत्र और ऊपर की ओर के क्षेत्र में एक स्वाभाविक तुलना बनती है, जिससे हमें जल प्रदूषण के आर्थिक प्रभाव के आकलन का तरीका मिलता है।
हम तीन प्रमुख पद्धतिगत चुनौतियों का समाधान करते हैं :
- i) बहुत ही कम या विरल निगरानी डेटा : दूषित जल में मौजूद विशिष्ट प्रदूषकों के प्रभाव को अलग करने के बजाय हम अत्यधिक प्रदूषणकारी औद्योगिक स्थलों के समग्र प्रभाव का अनुमान लगाते हैं। ऐसा करते हुए हम विभिन्न खामियोंसे भरपूर, अनियमित और पक्षपाती जल गुणवत्ता की निगरानी वाले डेटा को दरकिनार करते हैं।
- ii) जटिल प्रदूषण आवागमन : हम औद्योगिक स्थलों के सापेक्ष नदियों के ऊपरी और निचले क्षेत्रों के बेहतर मानचित्रण के लिए सटीक जल विज्ञान मॉडलों का उपयोग करते हैं।
iii) उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली फसल पैदावार की कमी : फसल की पैदावार को मापने के लिए, हम एनडीवीआई (सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक), ईवीआई (बढ़ी हुई वनस्पति सूचकांक) और अन्य सहित छह अलग-अलग उपग्रह जानकारी से तैयार वनस्पति सूचकांकों से पैदावार की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। भू-वैज्ञानिकों द्वारा विकसित ये सूचकांक, विभिन्न सेटिंगों में (रनिंग एवं अन्य 2004, बर्क और लोबेल 2017, लोबेल एवं अन्य 2022) फसल की पैदावार के विश्वसनीय भविष्यवक्ता हैं। गाँव-स्तरीय माइक्रो डेटा का उपयोग करके, हम कई मॉडलों को प्रशिक्षित करते हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मॉडल का चयन करते हैं। इस मॉडल में पहले के तरीकों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक सही भविष्यवाणी करने की शक्ति है।
शोध के परिणाम
पहली बड़ी बात यह है कि 'गम्भीर रूप से प्रदूषित' माने जाने वाले औद्योगिक स्थल भारी मात्रा में प्रदूषक जिनसे जल प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी होती है। आकृति-1 दर्शाता है कि इन स्थलों के नीचे की ओर का सतही जल प्रदूषण ऊपरी क्षेत्रों की तुलना में तीन से छह गुना बढ़ जाता है। इन स्थलों से प्रदूषण के इस पैमाने को पहले कभी सार्वजनिक रूप से मापा नहीं गया है।
आकृति-1. निगरानी स्टेशनों पर सतही जल प्रदूषण का माप

नोट : (i) ग्राफ़ औद्योगिक साइट से दूरी के क्वॉन्टाइल बिन में प्रत्येक पैरामीटर के औसत मानों को प्लॉट करते हैं। सकारात्मक दूरी यह बताती है कि साइट के नीचे की ओर एक निगरानी केन्द्र है और नकारात्मक का मतलब केन्द्र केन्द्र साइट के ऊपर की ओर है। पोलीनोमियल रेखाएँ दर्शाती हैं कि दूरी के साथ प्रदूषण कैसे बदल सकता है (ii) साइट पर प्रदूषण का अनुमानित प्रभाव प्रत्येक पैनल के अंदर मजबूत पी-मान (पी-वैल्यू) के साथ दर्ज किया गया है।
हमारा दूसरा मुख्य परिणाम आश्चर्यजनक है- प्रदूषित स्थलों के नीचे की ओर फसल की पैदावार ऊपर की ओर की तुलना में बहुत कम नहीं पाई गई है। आकृति-2 में पैदावार में 3% की मामूली गिरावट दिखाई गई है, लेकिन 95% विश्वास अंतराल में शून्य2 शामिल है। और हम उपज में 7% से अधिक की गिरावट को खारिज कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि फसल की पैदावार पर प्रदूषण का स्थानीयकृत प्रभाव भी छोटा है। ये प्रभाव संभवतः बहाव के नीचे की ओर और भी छोटे हैं, जहाँ प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है।
हालांकि, उन क्षेत्रों में उपज में बड़ी कमी देखी गई है जहाँ प्रदूषण का जोखिम अधिक है। जैसे कि नहरों द्वारा सिंचित गाँव, नदियों के पास के गाँव या वे गाँव जहाँ भूजल कम गहराई में मौजूद है जिससे प्रदूषण अधिक आसानी से रिस सकता है। उदाहरण के लिए, नहर से सिंचित गाँवों में उपज में, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण, 10% की गिरावट दिखती है, जैसा कि आकृति-2 के पैनल (बी) में दिखाया गया है।
आकृति-2. उपग्रह डेटा से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार गाँव में औसत फसल पैदावार

नोट : (i) ग्राफ औद्योगिक साइट से दूरी के क्वॉन्टाइल बिन में प्रत्येक पैरामीटर के औसत मूल्यों को प्लॉट करते हैं। सकारात्मक दूरी यह दर्शाती है कि साइट के नीचे की ओर एक निगरानी केन्द्र है, नकारात्मक का मतलब है कि केन्द्र साइट के ऊपर की ओर है। पोलीनोमियल रेखाएँ यह दर्शाती हैं कि दूरी के साथ फसल की पैदावार कैसे बदल सकती है (ii) साइट पर प्रदूषण का अनुमानित प्रभाव मजबूत पी-वैल्यू के साथ प्रत्येक पैनल में दर्ज है। (iii) पैनल (बी), (सी), (डी) गाँव के नमूने को सीमित करते हैं।
प्रभाव छोटे क्यों हैं?
तीन कारण यह समझाने में सहायक हैं कि प्रदूषण का कृषि उत्पादन पर समग्र रूप से बड़ा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है :
i) सीमित फसल जोखिम : सभी फसलें प्रदूषित पानी के सम्पर्क में नहीं आती हैं। उदाहरण के लिए, भूजल प्रदूषण पूरे नमूने में बहुत अधिक नहीं बढ़ता है।
ii) प्रदूषण का क्षीणन : जैसे-जैसे प्रदूषण आगे बढ़ता है, यह अवसादन, निस्पंदन और विसरण के माध्यम से क्षीण होता जाता है, जिससे खेतों तक पहुँचने तक इसकी सांद्रता यानी सेचुरेशन कम हो जाती है।
iii) लाभकारी घटक : औद्योगिक अपशिष्टों में कभी-कभी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो उर्वरक की तरह काम करते हैं। हमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि जो औद्योगिक स्थान अधिक पोषक तत्व छोड़ते हैं, उनका फसल की पैदावार पर कम प्रभाव पड़ता है।
हमने यह भी जांच की कि क्या किसान कृषि पद्धतियों में बदलाव करके प्रदूषण से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? जैसे कि अधिक उर्वरकों का उपयोग करना या सिंचाई के तरीकों में बदलाव करना। इनपुट में बदलाव के बहुत कम सबूत हैं और घरेलू खपत या गरीबी दरों पर इनका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है।
निष्कर्ष
हमने अध्ययन किया कि भारत में अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक स्थलों से होने वाला जल प्रदूषण कृषि उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है। ये स्थल नदी प्रदूषण में महत्वपूर्ण उछाल का कारण बनते हैं, लेकिन फसल की पैदावार पर इनका प्रभाव, आश्चर्यजनक रूप से कम होता है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि (i) अधिकांश फसलें सीधे प्रदूषण के सम्पर्क में नहीं आती हैं (ii) प्रदूषण खेतों तक पहुँचने से पहले ही कम हो जाता है और (iii) कुछ प्रदूषकों में ऐसे पोषक तत्व शामिल होते हैं जो फसलों को लाभ पहुँचाते हैं। यह निष्कर्ष विकसित दुनिया के अन्य शोध साहित्य के अनुरूप भी है जिसमें अधिकांश, जल प्रदूषण को साफ करने के बड़े गैर-स्वास्थ्य लाभ नहीं पाए जाते हैं (कीज़र और शापिरो 2019)।
हमारे निष्कर्ष का हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि औद्योगिक जल प्रदूषण हानिरहित है। कृषि पर इसका प्रभाव संभवतः बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र जैसे अन्य गम्भीर नुकसान हो सकते हैं। इन व्यापक प्रभावों को समझना भविष्य के शोध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
टिप्पणियाँ :
- अध्ययन के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है, जैसे कि जनगणना (2011), सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (2012), श्रग- एसएचआरयूजी (सामाजिक आर्थिक उच्च-रिज़ॉल्यूशन ग्रामीण-शहरी भौगोलिक प्लेटफ़ॉर्म) डेटाबेस, खेती की लागत पर कृषि मंत्रालय का सर्वेक्षण (2015-2018) और इसी तरह के अन्य स्रोत।
- 95% विश्वास अंतराल का मतलब है कि यदि आप नए नमूनों के साथ प्रयोग को बार-बार दोहराते हैं, तो 95% समय पर सीआई गणना में सटीक प्रभाव होगा। सीआई जिनमें शून्य शामिल नहीं होता, 5% स्तर पर सांख्यिकीय महत्व को दर्शाता है।
अंग्रेज़ी के मूल लेख और संदर्भों की सूची के लिए कृपया यहां देखें।
लेखक परिचय : निकोलस हेगर्टी मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी में कृषि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उनका शोध इस बात का अध्ययन करता है कि दुनिया भर के समाज पर्यावरणीय परिवर्तन से कैसे निपटते हैं और कैसे नीति डिज़ाइन लोगों को बेहतर ढंग से अनुकूलित करने में मदद कर सकता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों की क्या भूमिका है। उन्होंने एमआईटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और यूसी बर्कले में एसवी सिरियासी-वांट्रप पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप की है। उन्होंने जे-पीएएल और आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए भी काम किया है। अंशुमान तिवारी भारत स्थित शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर हैं। इससे पहले, वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में पर्यावरण बाज़ार प्रयोगशाला में पोस्ट डॉक्टरल फेलो थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पर्यावरण अर्थशास्त्र में पीएचडी, यूसी बर्कले से पब्लिक पॉलिसी में मास्टरस डिग्री और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम धनबाद) से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आते हैं? नए पोस्टों की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम (@I4I_Hindi) चैनल से जुड़ें। इसके अलावा हमारे मासिक न्यूज़ लेटर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दायीं ओर दिए गए फॉर्म को भरें।




 05 जून, 2025
05 जून, 2025 


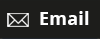


Comments will be held for moderation. Your contact information will not be made public.